माया को समझना: वास्तविकता के भ्रम का अनावरण
नमस्ते। त्रिदिवसीय त्रिज्ञान कार्यक्रम के इस दूसरे दिन में आपका स्वागत है। आज हम “माया के ज्ञान” पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसे “जगत का ज्ञान” भी कहा जाता है। यह सत्र आपको माया को समझने में मदद करेगा और यह जानने में मदद करेगा कि जिसे हम यथार्थ समझते हैं, वह वास्तव में क्या है।
माया क्या है?
माया शब्द का अर्थ है “जो नहीं है”। संस्कृत में ‘मा’ का अर्थ है ‘नहीं’ और ‘या’ का अर्थ है ‘जो है’। इस प्रकार, माया वह है जो प्रतीत तो होती है, पर जिसका वास्तविक और स्थायी अस्तित्व नहीं है। इसे एक प्रकार की लीला या खेल भी कहा जा सकता है। यह अवधारणा हमारी उस अंतर्निहित धारणा को चुनौती देती है कि हमारे आसपास की दुनिया ठोस और स्थायी है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि हमारी इंद्रियां हमें दुनिया के बारे में सटीक जानकारी देती हैं। माया का विचार इस स्थापित विश्वास को हिला देता है और हमें वास्तविकता की प्रकृति पर गहराई से विचार करने के लिए प्रेरित करता है।
मुख्य बात यह है कि माया वह है जिसका अनुभव तो होता है, पर वह परम सत्य नहीं है। इसे समझने के लिए एक सरल उदाहरण लेते हैं: रेगिस्तान में मरीचिका। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि पानी का जलाशय है, लेकिन जब आप वहां पहुंचते हैं, तो आपको पता चलता है कि वह केवल गर्मी के कारण उत्पन्न हुआ एक भ्रम था। इसी तरह, माया के संदर्भ में, हमारे रोजमर्रा के अनुभव, जो हमें बहुत वास्तविक लगते हैं, एक बड़े अर्थ में भ्रम हो सकते हैं।
जो भी हमें दिखाई, सुनाई या महसूस होता है, वह वैसा नहीं है जैसा वह प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए, आपके सामने एक टेबल रखा है। आपको टेबल दिखाई दे रहा है, आप उसे हाथों से छूकर भी महसूस कर सकते हैं। लेकिन क्या वह वास्तव में वैसा ही है जैसा आप अनुभव कर रहे हैं? हमारी इंद्रियां हमें जो संकेत दे रही हैं, हम उतना ही जान पाते हैं। सूक्ष्म स्तर पर देखें तो यह टेबल परमाणुओं और अणुओं से बना है जो लगातार गतिमान हैं और जिनके बीच में बहुत सारा खाली स्थान है। हमारी इंद्रियां हमें इस सूक्ष्म वास्तविकता का अनुभव नहीं करा पाती हैं, बल्कि एक स्थूल और स्थिर वस्तु का अनुभव कराती हैं।
जगत माया क्यों है?
हमने कल आत्मज्ञान में समझा था कि सत्य वह है जो कभी परिवर्तित नहीं होता – न समय के अनुसार, न स्थिति के अनुसार और न ही अवस्थाओं के अनुसार। जो भी वस्तु या अनुभव बदलता है, वह सत्य नहीं हो सकता, वह मिथ्या या माया है। अपरिवर्तनीय सत्य की यह अवधारणा हमें परिवर्तनशील जगत के संदर्भ में एक स्थिर आधार प्रदान करती है। यदि हमारे आसपास सब कुछ बदल रहा है, तो क्या कुछ ऐसा है जो स्थायी है?
परिवर्तनशीलता:
यह जगत, हमारा शरीर, हमारी भावनाएं, सब कुछ निरंतर बदल रहा है। जो बदल रहा है, वह झूठ है, मिथ्या है। उदाहरण के लिए, आप बाजार से कोई वस्तु ₹50 में खरीदते हैं, अगले दिन उसकी कीमत बदल सकती है। आपका नाम आज विजय है, कल कुछ और हो सकता है। ये सब परिवर्तनशील हैं। इसके अतिरिक्त, मौसम बदलते रहते हैं, एक पौधा बढ़ता और बूढ़ा होता है, और हमारी भावनाएं पल-पल बदलती रहती हैं। इन सभी उदाहरणों में, हम परिवर्तन की एक सतत प्रक्रिया देखते हैं, जो माया की क्षणभंगुर प्रकृति को दर्शाती है।
यहां तक कि सूर्य, चंद्र, पृथ्वी भी बदल रहे हैं, यद्यपि उनकी गति बहुत धीमी है। पहाड़ मैदान बन जाते हैं, और मैदानों की जगह पहाड़ आ सकते हैं। आपका शरीर बचपन से अब तक कितना बदल गया है, और भविष्य में भी बदलेगा। यदि हम दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखें, तो हमें पता चलता है कि ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है। हमारी धारणा में जो चीजें स्थायी लगती हैं, वे भी समय के साथ धीरे-धीरे बदल रही हैं। यह दीर्घकालिक परिवर्तन हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी अल्पकालिक धारणाएं हमें स्थायित्व का भ्रम दे सकती हैं।
इंद्रियों पर निर्भरता:
हम जगत का अनुभव अपनी पांच भौतिक इंद्रियों (आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा) के माध्यम से करते हैं। जो ज्ञान हमें इंद्रियों से मिलता है, वह सीमित और परिवर्तनशील होता है। हमारी इंद्रियां वास्तविकता को सीधे तौर पर अनुभव नहीं करती हैं, बल्कि बाहरी उत्तेजनाओं को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करती हैं, जिन्हें हमारा मस्तिष्क व्याख्या करता है। इस प्रक्रिया में, जानकारी का कुछ अंश खो सकता है या विकृत हो सकता है।
- उदाहरण (आंखें): आपको एक ट्यूबलाइट से सफेद रोशनी दिखाई दे रही है। यह इसलिए सत्य लग रही है क्योंकि आपकी आंखें उसे देख रही हैं। अगर आंखें न हों, या आप आंखें बंद कर लें, तो वह रोशनी कहां है? अब यदि आप एक लाल रंग का चश्मा पहन लें, तो वही सफेद रोशनी आपको लाल दिखाई देने लगेगी। इसका अर्थ है कि रंग वस्तु (रोशनी) में नहीं, बल्कि आपकी आंखों और देखने के माध्यम (चश्मा) पर निर्भर करता है। वास्तव में जगत में कोई स्थायी रंग नहीं है। विभिन्न प्रकाश स्थितियों (जैसे दिन का उजाला बनाम कृत्रिम प्रकाश) के तहत एक ही वस्तु अलग-अलग रंग की दिख सकती है। यह इस बात पर और जोर देता है कि रंग वस्तु का एक अंतर्निहित गुण नहीं है, बल्कि प्रकाश, वस्तु और हमारी देखने की प्रक्रिया के बीच एक अंतःक्रिया का परिणाम है।
- एक और उदाहरण: एक व्यक्ति जिसे रंगों को पहचानने में समस्या है (कलर ब्लाइंडनेस), उसके लिए ट्रैफिक सिग्नल के लाल रंग का अर्थ कुछ और हो सकता है। तो सत्य क्या है? कभी-कभी हमें दृष्टिभ्रम भी होता है, जैसे कमरे में किसी के होने का भ्रम, जबकि वहां कोई नहीं होता। यह दर्शाता है कि हमारी दृश्य धारणा व्यक्तिपरक हो सकती है और बाहरी परिस्थितियों और हमारी अपनी शारीरिक स्थितियों से प्रभावित हो सकती है।
- उदाहरण (स्पर्श/त्वचा): यदि आप एक हाथ बहुत गर्म पानी में और दूसरा बहुत ठंडे बर्फीले पानी में कुछ देर रखते हैं, और फिर दोनों हाथों को एक साथ सामान्य तापमान वाले पानी के बर्तन में डालते हैं, तो गर्म पानी से निकले हाथ को सामान्य पानी ठंडा लगेगा, और ठंडे पानी से निकले हाथ को वही सामान्य पानी गर्म महसूस होगा। पानी तो वही है, पर अनुभव अलग-अलग है। यह दिखाता है कि ठंडा-गर्म का अनुभव भी हमारी इंद्रियों की स्थिति पर निर्भर करता है, वस्तु का स्थायी गुण नहीं है। इसी प्रकार, यदि कोई व्यक्ति ठंडे मौसम से गर्म कमरे में प्रवेश करता है, तो कमरा उसे बहुत गर्म लग सकता है, जबकि कमरे में रहने वाले अन्य लोगों को वह सामान्य लग सकता है। यह हमारी त्वचा की अनुकूलन क्षमता को दर्शाता है और यह कि हमारी स्पर्श संबंधी संवेदनाएं निरपेक्ष नहीं बल्कि सापेक्ष होती हैं।
- उदाहरण (स्वाद/जीभ): भोजन में स्वाद हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जो भोजन आज आपको बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, वही भोजन जब आपको बुखार आता है या आपकी जीभ का स्वाद बदल जाता है, तो बेस्वाद या कड़वा लग सकता है। यदि स्वाद भोजन का स्थायी गुण होता, तो वह हर अवस्था में वैसा ही लगता। इसके अतिरिक्त, एक ही भोजन अलग-अलग लोगों को अलग-अलग स्वाद का लग सकता है। कुछ लोगों को धनिया का स्वाद बहुत अच्छा लगता है, जबकि कुछ लोगों को वह साबुन जैसा लगता है। यह व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और आनुवंशिक कारकों के प्रभाव को दर्शाता है।
- उदाहरण (गंध/नाक): किसी को एक विशेष सुगंध बहुत अच्छी लग सकती है, जबकि दूसरे व्यक्ति को वही सुगंध सामान्य या बुरी लग सकती है। कुछ लोगों को तो कुछ विशेष गंध आती ही नहीं है। तो क्या सुगंध वस्तु में है या हमारी नाक की ग्रहण करने की क्षमता और हमारी पसंद-नापसंद पर निर्भर है? किसी विशेष गंध से जुड़ी हमारी यादें भी हमारी प्रतिक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, बचपन में किसी अप्रिय घटना से जुड़ी गंध बड़े होने पर भी नकारात्मक भावनाएं पैदा कर सकती है।
माया हमें सत्य क्यों लगती है?
यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगर यह जगत माया है, तो यह हमें इतना वास्तविक क्यों लगता है? इसके कुछ कारण हैं:
परिवर्तन की धीमी गति:
जिन वस्तुओं में परिवर्तन की गति बहुत धीमी होती है, वे हमें स्थायी और सत्य प्रतीत होती हैं। उदाहरण: एक कुर्सी जो 10-15 साल तक चलती है, हमें स्थायी लगती है। एक टमाटर जो कुछ दिनों में सड़ जाता है, वह अनित्य लगता है। यदि हम समय की गति को बहुत तेज कर दें, तो 10 साल तक चलने वाली कुर्सी भी कुछ ही सेकंड में पुरानी होकर नष्ट होती हुई दिखाई देगी, और तब वह उतनी सत्य नहीं लगेगी। इसी प्रकार, टमाटर यदि कुछ सेकंड में ही रखकर गायब हो जाए, तो हमें उसके अस्तित्व पर ही संदेह होगा। हमारी समय की सीमित धारणा के कारण, हम उन परिवर्तनों को नहीं देख पाते हैं जो धीरे-धीरे होते हैं, जिससे हमें स्थायित्व का भ्रम होता है।
स्मृति (याददाश्त):
हमारी स्मृति भी वस्तुओं और अनुभवों को स्थायित्व प्रदान करती है। उदाहरण: हमें बचपन से सिखाया जाता है कि नीले रंग को ‘नीला’ कहते हैं। यह हमारी स्मृति में बैठ जाता है। अगर बचपन से ही आपको नीले रंग को ‘सफेद’ सिखाया जाता, तो आप आज उसे सफेद ही कह रहे होते। इसी तरह, किसी वस्तु (जैसे कुर्सी) का एक निश्चित आकार-प्रकार हमारी स्मृति में होता है, जिससे हम उसे पहचानते हैं। यदि वह स्मृति हटा दी जाए, तो हम उस वस्तु को नहीं पहचान पाएंगे। हमारी यादें हमें दुनिया का एक स्थिर मानसिक मॉडल बनाने में मदद करती हैं, भले ही वास्तविक भौतिक वास्तविकता लगातार बदल रही हो।
वस्तुनिष्ठता का भ्रम (Objective Reality) / सामूहिक सहमति:
जब कई लोग एक ही चीज़ का अनुभव करते हैं और उसे एक ही नाम से जानते हैं (जैसे टेबल), तो हमें वह चीज़ सत्य लगने लगती है। हम सोचते हैं कि क्योंकि दूसरे भी इसे देख रहे हैं या मान रहे हैं, इसलिए यह सच है। लेकिन यह केवल साझा अनुभव या सहमति है, परम सत्य नहीं। उदाहरण: यदि एक व्यक्ति कहता है कि टेबल लाल रंग का है और दूसरा कहता है कि वह हरे रंग का है, तो भ्रम उत्पन्न होता है। लेकिन यदि समाज के अधिकांश लोग एक बात पर सहमत हो जाएं, तो उसे सत्य मान लिया जाता है, भले ही वह बदलता रहे। पैसे का उदाहरण लें। इसका मूल्य सामूहिक विश्वास और समझौते पर आधारित है। यदि वह विश्वास गायब हो जाए, तो पैसा केवल कागज या धातु का टुकड़ा बन जाएगा। यह दर्शाता है कि हमारी सामाजिक और आर्थिक वास्तविकता के कई पहलू साझा समझौतों और मान्यताओं पर निर्मित हैं।
अनुभव और अनुभवकर्ता
जो भी अनुभव हो रहा है (दृश्य, श्रव्य, गंध, स्वाद, स्पर्श), वह माया है क्योंकि वह बदल रहा है और इंद्रियों पर निर्भर है। लेकिन “अनुभवकर्ता” – वह जो इन अनुभवों को जान रहा है, यानी “मैं” या “आप” – वह सत्य है। अनुभवकर्ता बदल नहीं रहा; अनुभव बदल रहे हैं। आपका अस्तित्व है, यह अटल सत्य है। अनुभवों के लगातार बदलते रहने के बावजूद, एक स्थिर जागरूकता है जो इन परिवर्तनों को देख रही है।
ज्ञान मार्ग के अनुसार, जो बदल जाता है, उस पर शंका होती है कि वह सच है या नहीं। हमारे सारे अनुभव बदलते हैं। केवल अनुभवकर्ता ही ऐसा है जिसके अस्तित्व के बारे में पक्का कहा जा सकता है कि वह है। बाकी सब आना-जाना है। यह परिप्रेक्ष्य हमें उन चीजों की परम वास्तविकता पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है जो परिवर्तन के अधीन हैं और हमारे होने के अपरिवर्तनीय सार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है।
अन्य उदाहरण:
- सपना: जब हम सपना देखते हैं, तो सपने में घटने वाली घटनाएं, लोग, वस्तुएं सब कुछ वास्तविक लगते हैं। हम सपने में डरते हैं, खुश होते हैं। लेकिन आंख खुलने पर पता चलता है कि वह सब मिथ्या था, हमारी अपनी कल्पना थी। कुछ देर बाद हम सपना भूल भी जाते हैं। सपने की दुनिया हमारी जागृत अवस्था की वास्तविकता का एक शक्तिशाली समानांतर प्रस्तुत करती है, यह दर्शाती है कि मन ऐसी वास्तविकताएं बना सकता है जिनमें कोई स्थायी पदार्थ नहीं होता है।
- सिनेमा/फिल्म: जैसे हम सिनेमा हॉल में फिल्म देखते हैं, पर्दे पर चित्र चलते हैं, कहानी आगे बढ़ती है, हम उसमें पूरी तरह डूब जाते हैं – कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी गुस्सा करते हैं। उस समय वह सब कुछ वास्तविक लगता है। लेकिन जैसे ही फिल्म खत्म होती है, हमें एहसास होता है कि वह सब माया थी, पर्दे पर दिखाया गया एक भ्रम था। कुछ लोग फिल्म के प्रभाव में इतने खो जाते हैं कि बाहर आकर भी उसी की चर्चा करते हैं और उसे सच मानते हैं। फिल्म देखने का अनुभव हमारी उस क्षमता को उजागर करता है कि हम एक निर्मित वास्तविकता में पूरी तरह से तल्लीन हो सकते हैं और उसकी क्षणभंगुर प्रकृति को भूल सकते हैं।
- बच्चों का कार्टून देखना: छोटे बच्चे जब कार्टून देखते हैं, तो उन्हें कार्टून के पात्र और घटनाएं बिल्कुल सच्ची लगती हैं। यदि कोई उन्हें कहे कि यह झूठ है, तो वे विश्वास नहीं करते। बड़े होने पर, बुद्धि विकसित होने पर समझ आता है कि वह काल्पनिक था। यह प्रक्रिया दिखाती है कि हमारी वास्तविकता की धारणा हमारी समझ और परिपक्वता के साथ कैसे विकसित होती है।
सत्य क्या है और यह भ्रम क्यों?
सत्य अपरिवर्तनशील है: जो सत्य है, वह कभी नहीं बदलता – न समय के प्रभाव से, न स्थिति के प्रभाव से, और न ही किसी अवस्था के बदलने से।
बदलने वाला झूठ है: जो कुछ भी बदल रहा है, वह झूठ है, मिथ्या है, माया है।
भ्रम का कारण:
- इंद्रियों की सीमाएं: हमारी इंद्रियां हमें सीमित और सापेक्ष ज्ञान देती हैं। हमारी इंद्रियां वास्तविकता का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान नहीं करती हैं, बल्कि एक सीमित और व्यक्तिपरक दृष्टिकोण प्रदान करती हैं।
- परिवर्तन की धीमी गति: जैसा पहले बताया, धीमी गति से होने वाले परिवर्तन हमें स्थायित्व का भ्रम देते हैं। हम उन परिवर्तनों को देखने में विफल रहते हैं जो धीरे-धीरे होते हैं, जिससे हमें लगता है कि चीजें स्थिर हैं।
- स्मृति: हमारी यादें हमें वस्तुओं और अनुभवों को वास्तविक मानने में मदद करती हैं। हमारी यादें एक सतत कथा बनाती हैं जो हमें दुनिया को स्थिर और सुसंगत मानने के लिए प्रेरित करती है।
- अज्ञान/अविवेक: बुद्धि का सही उपयोग न होने के कारण हम माया को सत्य मान लेते हैं। वास्तविकता की गहरी समझ की कमी के कारण, हम अपनी इंद्रियजन्य धारणाओं और सीखी हुई मान्यताओं को अंतिम सत्य मान लेते हैं।




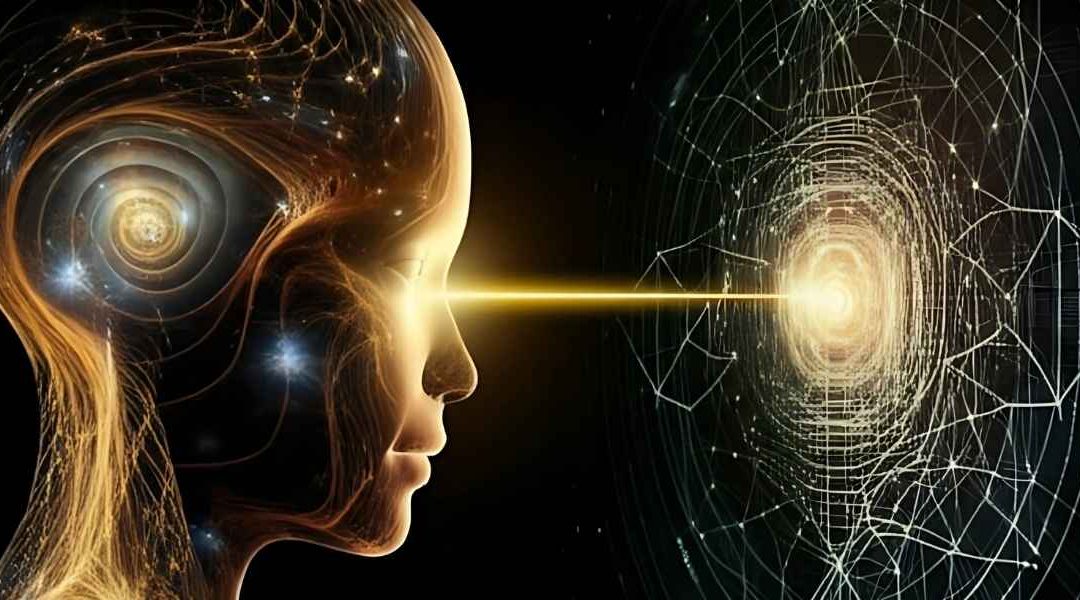

0 Comments