संसार में रहकर वैराग्य: गृहस्थ साधक की सबसे बड़ी चुनौती
ईशावास्य उपनिषद का प्रथम मंत्र “ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्” हमें यह स्पष्ट संदेश देता है कि समस्त जगत में ईश्वर का वास है। यह सूत्र आधुनिक साधकों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है – यदि सब कुछ में ईश्वर है, तो क्या संसार का त्याग आवश्यक है? क्या गृहस्थ धर्म और वैराग्य परस्पर विरोधी हैं?
आज के युग में अधिकांश साधक इस दुविधा में फंसे रहते हैं कि पारिवारिक दायित्वों, सामाजिक कर्तव्यों और आध्यात्मिक प्रगति के बीच संतुलन कैसे बनाएं। वैराग्य के नाम पर संसार से पूर्ण विमुखता की परंपरागत धारणा ने इस भ्रम को और भी गहरा कर दिया है।
वास्तविकता यह है कि वेदांत शास्त्र में वैराग्य का अर्थ संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए आसक्ति से मुक्त होना है। यही वह मार्ग है जिसे श्रीमद्भगवद्गीता में निष्काम कर्म योग के नाम से प्रतिष्ठित किया गया है।
वैराग्य का शास्त्रीय अर्थ
पतंजलि योग सूत्र में वैराग्य की परिभाषा करते हुए कहा गया है – “दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्”। इसका अर्थ है कि दृश्य और अदृश्य विषयों में से तृष्णा का नाश हो जाना ही वैराग्य है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि वैराग्य विषयों का त्याग नहीं, बल्कि विषयों में तृष्णा का त्याग है।
आदि शंकराचार्य ने अपनी टीकाओं में स्पष्ट किया है कि वैराग्य राग का विलोम है, न कि भोग का। राग का अर्थ है आसक्ति, लगाव, और मोह। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के साथ इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि उसके बिना हमारी प्रसन्नता असंभव लगने लगती है, तो यही राग है।
संत कबीर दास जी ने इस सत्य को अपने सहज भाव में व्यक्त किया है – “कबीरा खड़ा बाज़ार में, मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर।” यह दोहा वैराग्य की सर्वोत्तम परिभाषा है – संसार में रहते हुए समभाव।
श्रीमद्भगवद्गीता में श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा है – “कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि।” यह श्लोक निष्काम कर्म योग का मूल सूत्र है, जो गृहस्थ धर्म में वैराग्य का आधार स्तंभ है।
गृहस्थ धर्म में वैराग्य के आयाम
कर्म क्षेत्र में निष्काम भाव
कर्म क्षेत्र में वैराग्य का अर्थ है अपने कर्तव्यों का पालन करते समय फल की आसक्ति से मुक्त रहना। गीता में स्पष्ट कहा गया है – “योगः कर्मसु कौशलम्” – कर्म में कुशलता ही योग है। यहाँ कुशलता का अर्थ केवल दक्षता नहीं, बल्कि आसक्ति रहित भाव से कर्म करना है।
यज्ञावल्क्य स्मृति में गृहस्थ के कर्तव्यों का विस्तृत वर्णन करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि गृहस्थ अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए भी परम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। आवश्यकता केवल दृष्टिकोण की शुद्धता की है।
कर्म क्षेत्र में वैराग्य का व्यावहारिक अर्थ है:
- अपना सर्वोत्तम प्रयास करना लेकिन परिणाम की चिंता न करना
- सफलता-असफलता में समान भाव रखना
- कर्म को ईश्वर की सेवा मानकर करना
- अहंकार भाव से मुक्त होकर कर्म करना
पारिवारिक संबंधों में स्नेह-अनासक्ति
तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है – “मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव”। इससे स्पष्ट होता है कि वैदिक परंपरा में पारिवारिक संबंधों को दैवीय भाव से देखा गया है। वैराग्य का अर्थ पारिवारिक प्रेम का त्याग नहीं, बल्कि उसमें दैवीय भाव का समावेश है।
स्नेह और आसक्ति के बीच सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। स्नेह निस्वार्थ होता है, आसक्ति स्वार्थ से भरी होती है। स्नेह देता है, आसक्ति लेना चाहती है। स्नेह स्वतंत्रता देता है, आसक्ति बांधती है।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है – “सिय राममय सब जग जानी, करउं प्रणाम जोरि जुग पानी”। यह भाव वैराग्य की पराकाष्ठा है – जब हम सभी में राम तत्व का दर्शन करने लगते हैं।
पारिवारिक संबंधों में वैराग्य का अर्थ:
- परिवारजनों से प्रेम करना लेकिन उन्हें नियंत्रित करने की इच्छा न रखना
- उनकी प्रसन्नता चाहना लेकिन उनकी प्रसन्नता पर अपनी प्रसन्नता आधारित न करना
- उनकी सेवा करना लेकिन कृतज्ञता की अपेक्षा न रखना
- उन्हें मार्गदर्शन देना लेकिन अपनी राय थोपना नहीं
भौतिक साधनों के साथ न्यूनतावाद
छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है – “अनन्नन्न पुरुषो वै सन्धायाम्” – अन्न के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। यह सूत्र इस सत्य को प्रकट करता है कि भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन अनावश्यक संग्रह आध्यात्मिक प्रगति में बाधक है।
गीता में श्रीकृष्ण कहते हैं – “युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु। युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा।” संतुलित आहार-विहार, संतुलित कर्म, संतुलित निद्रा-जागरण योग के लिए आवश्यक है।
आवश्यकता और इच्छा का विवेक
वैराग्य का व्यावहारिक पहलू यह समझना है कि क्या आवश्यकता है और क्या केवल इच्छा है। आवश्यकता वह है जो जीवन यापन के लिए आवश्यक है, इच्छा वह है जो सुविधा या दिखावे के लिए चाहिए।
यातायात साधन का उदाहरण: यदि आप ऐसे स्थान पर निवास करते हैं जहाँ सार्वजनिक यातायात उपलब्ध नहीं है और आपको नियमित यातायात की आवश्यकता है, तो व्यक्तिगत वाहन रखना उचित है। परंतु यदि मासिक उपयोग अत्यंत सीमित है, तो विकल्पों की खोज करना वैराग्य है।
मुख्य सिद्धांत:
- आवश्यकता के अनुसार निर्णय लेना, सामाजिक दिखावे के अनुसार नहीं
- एकाधिक साधनों की वास्तविक आवश्यकता का ईमानदारी से मूल्यांकन
- गुणवत्ता को प्राथमिकता देना, मात्रा को नहीं
- दीर्घकालिक लाभ को देखना, तात्कालिक संतुष्टि को नहीं
आंतरिक वैराग्य के सोपान
साक्षी भाव का विकास
अष्टावक्र गीता में कहा गया है – “साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च”। साक्षी भाव वैराग्य की आधारशिला है। यह वह अवस्था है जहाँ हम अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को एक तटस्थ दृष्टा के रूप में देखते हैं।
रमण महर्षि ने “मैं कौन हूं?” की विधि के माध्यम से साक्षी भाव के विकास का सरल उपाय बताया है। यह विधि दैनिक जीवन में निरंतर अभ्यास की जा सकती है।
साक्षी भाव के व्यावहारिक अभ्यास:
- कार्य करते समय यह देखना कि कौन कार्य कर रहा है
- भावनाओं के उठने पर यह देखना कि कौन अनुभव कर रहा है
- विचारों की धारा को देखना, उनमें बह न जाना
- श्वास की गति को देखना, उसे नियंत्रित करने का प्रयास न करना
अनित्यता बोध
कठोपनिषद में स्पष्ट कहा गया है – “सर्वं खल्विदं ब्रह्म, नेह नानास्ति किंचन”। यह सूत्र अनित्यता के बोध को स्थापित करता है। जब हम यह समझ जाते हैं कि सब कुछ परिवर्तनशील है, तो आसक्ति स्वयं ही छूटने लगती है।
ओशो के शब्दों में – “परिवर्तन ही जीवन का एकमात्र स्थायी तत्व है।” इस सत्य को जीवन में उतारना वैराग्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
अनित्यता बोध के अभ्यास:
- प्रतिदिन यह चिंतन करना कि कल जो था, आज नहीं है
- अपने बचपन की स्मृतियों को देखकर समझना कि सब कुछ बदल गया है
- प्रकृति में होने वाले चक्रीय परिवर्तनों को देखना
- अपने विचारों और भावनाओं की अस्थायित्व को देखना
आत्म विचार
मुंडकोपनिषद में कहा गया है – “एतमात्मानं विदित्वा सर्वपाशैर्विमुच्यते”। आत्मा को जानकर सभी बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। आत्म विचार वैराग्य का चरम लक्ष्य है।
आत्म विचार का अर्थ है अपनी वास्तविक पहचान की खोज करना। हम देह हैं या देह से अतिरिक्त कुछ और हैं? हम मन हैं या मन के दृष्टा हैं? हम बुद्धि हैं या बुद्धि के साक्षी हैं?
आचार्य प्रशांत के अनुसार, “आत्मा की शुद्धता में स्थिति ही वैराग्य है।” जब हम अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तो बाहरी आकर्षण अपनी शक्ति खो देते हैं।
आत्म विचार की विधि:
- प्रतिदिन कुछ समय मौन में बैठकर “मैं कौन हूं?” पूछना
- देह की संवेदनाओं को देखते हुए यह अनुभव करना कि मैं देह का दृष्टा हूं
- मन के विचारों को देखते हुए यह अनुभव करना कि मैं मन का साक्षी हूं
- भावनाओं के उठने-गिरने को देखते हुए यह जानना कि मैं भावनाओं से अतिरिक्त हूं
गुरु मार्गदर्शन का महत्व
श्वेताश्वतरोपनिषद में कहा गया है – “यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ। तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः।” गुरु में देव तुल्य भक्ति रखने वाले को ही परम सत्य का बोध होता है।
स्वाध्याय और गुरु शिक्षा के बीच मूलभूत अंतर है। स्वाध्याय से ज्ञान मिलता है, गुरु से बोध मिलता है। ज्ञान बौद्धिक होता है, बोध अनुभवजन्य होता है।
संत कबीर ने गुरु की महिमा का गुणगान करते हुए कहा है – “गुरु गोविन्द दोनों खड़े, काके लागूं पाय। बलिहारी गुरु आपने, गोविन्द दियो बताय।” यह दोहा गुरु की महत्ता को प्रकट करता है।
वैराग्य के मार्ग में गुरु का महत्व:
- वैराग्य और उदासीनता के बीच अंतर स्पष्ट करना
- व्यावहारिक जीवन में वैराग्य के सिद्धांतों को लागू करने की विधि बताना
- साधना में आने वाली कठिनाइयों का समाधान देना
- आध्यात्मिक अनुभवों की सही व्याख्या करना
- व्यक्तिगत प्रकृति के अनुसार साधना पद्धति निर्धारित करना
अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में वैराग्य का विकास द्रुत गति से होता है। गुरु के पास वह प्रज्ञा होती है जो शास्त्रों के अध्ययन और व्यावहारिक अनुभव दोनों से प्राप्त होती है।
सामान्य बाधाएं और समाधान
पारिवारिक विरोध
अक्सर गृहस्थ साधकों को परिवार से यह शिकायत सुनने को मिलती है कि वे अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहे हैं। इस स्थिति में गीता का यह श्लोक मार्गदर्शन देता है – “सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज”।
यहाँ धर्म का अर्थ धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि सामाजिक कर्तव्य है। श्रीकृष्ण का संदेश यह है कि सभी कर्तव्यों का पालन ईश्वर की शरण में करना चाहिए।
समाधान:
- परिवारजनों को समझाना कि वैराग्य प्रेम का विरोधी नहीं है
- अपने व्यवहार में परिवर्तन दिखाना, केवल शब्दों से नहीं
- पारिवारिक दायित्वों का और भी बेहतर निर्वाह करना
- धैर्य रखना और समय देना
कर्म में उदासीनता
वैराग्य की गलत समझ से कभी-कभी साधक कर्म में उदासीनता दिखाने लगते हैं। गीता में इसका स्पष्ट निवारण मिलता है – “योगः कर्मसु कौशलम्”।
निष्काम कर्म का अर्थ कर्म न करना नहीं, बल्कि कुशलता से कर्म करना है। वैराग्य कर्म की गुणवत्ता बढ़ाता है, घटाता नहीं।
समाधान:
- कर्म को ईश्वर की पूजा मानकर करना
- सर्वोत्तम प्रयास करना लेकिन परिणाम ईश्वर पर छोड़ना
- कर्म में मन को पूर्णतः संलग्न करना
- कर्म के माध्यम से आत्म शुद्धि का भाव रखना
सामाजिक दायित्वों का संघर्ष
मनुस्मृति में गृहस्थ आश्रम के नियमों का विस्तृत वर्णन मिलता है। सामाजिक दायित्वों का निर्वाह गृहस्थ धर्म का अभिन्न अंग है।
वैराग्य का अर्थ सामाजिक दायित्वों से भागना नहीं है। वैराग्य तो उन दायित्वों को और भी बेहतर तरीके से निभाने की प्रेरणा देता है।
समाधान:
- सामाजिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी लेना
- जरूरतमंदों की सेवा को वैराग्य का अभ्यास मानना
- समाज कल्याण के कार्यों में योगदान देना
- संतुलित दृष्टिकोण रखना – न अतिवाद, न निष्क्रियता
महान गृहस्थ वैरागी परंपरा
राजा जनक: विदेह राज ऋषि
राजा जनक वैराग्य के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। उन्होंने राज्य का संचालन करते हुए परम ज्ञान की प्राप्ति की। उनका जीवन इस सत्य का प्रमाण है कि गृहस्थ धर्म और परम ज्ञान परस्पर विरोधी नहीं हैं।
योग वासिष्ठ में राजा जनक के जीवन का विस्तृत वर्णन मिलता है। उन्होंने कहा था – “मैं मिथिला का राजा हूं, परंतु मिथिला मेरी नहीं है।” यही वैराग्य है।
भर्तृहरि: त्याग और पुनः गृहस्थ
राजा भर्तृहरि ने पहले राज्य का त्याग करके संन्यास लिया, फिर गुरु के निर्देश पर पुनः गृहस्थ बने। उनका जीवन इस सत्य को प्रकट करता है कि वैराग्य बाहरी परिस्थितियों में नहीं, आंतरिक भाव में है।
तुकाराम: साधारण जीवन में असाधारण वैराग्य
संत तुकाराम ने एक साधारण किसान का जीवन जीते हुए परम ज्ञान की प्राप्ति की। उनके अभंग वैराग्य और गृहस्थ धर्म के मधुर संयोजन के उत्कृष्ट उदाहरण हैं।
इन महान आत्माओं का जीवन आधुनिक गृहस्थ साधकों के लिए प्रेरणास्रोत है। ये सिद्ध करते हैं कि संसार में रहकर भी संसार से मुक्त हुआ जा सकता है।
वैराग्य के चिह्न और फल
योग वासिष्ठ में जीवन्मुक्त के लक्षणों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वैराग्य प्राप्त व्यक्ति में निम्नलिखित चिह्न दिखाई देते हैं:
मानसिक शांति और स्थिरता
वैराग्य का प्रथम फल मानसिक शांति है। जब आसक्ति छूट जाती है, तो चित्त स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। पतंजलि ने कहा है – “ततः द्वन्द्वानभिघातः” – वैराग्य से द्वंद्वों का प्रभाव समाप्त हो जाता है।
संबंधों में सुधार
वैराग्य व्यक्ति के संबंधों को और भी मधुर बनाता है। जब हम दूसरों से कुछ पाने की अपेक्षा नहीं रखते, तो हमारा प्रेम निस्वार्थ हो जाता है। निस्वार्थ प्रेम ही सच्चा प्रेम है।
कार्यक्षमता में वृद्धि
वैराग्य कार्यक्षमता को कम नहीं, बल्कि बढ़ाता है। जब परिणाम की चिंता नहीं रहती, तो पूरी ऊर्जा कर्म में लग जाती है। यही कारण है कि वैरागी व्यक्ति अधिक कुशलता से कार्य करता है।
आध्यात्मिक प्रगति
वैराग्य आध्यात्मिक प्रगति का द्वार है। जब मन बाहरी विषयों में उलझा नहीं रहता, तो वह स्वयं अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाता है। यही समाधि की अवस्था है।
दैनिक साधना में वैराग्य
प्रातःकाल: आत्म चिंतन और संकल्प
प्रतिदिन प्रातःकाल कुछ समय आत्म चिंतन के लिए निकालना आवश्यक है। इस समय यह संकल्प करना चाहिए कि आज का दिन वैराग्य भाव से जिया जाएगा।
गीता का स्वाध्याय विशेष रूप से लाभकारी है। गीता के श्लोकों में वैराग्य के व्यावहारिक सूत्र भरे पड़े हैं।
प्रातःकालीन अभ्यास:
- मौन में बैठकर “मैं कौन हूं?” का चिंतन
- दिन भर के कार्यों को ईश्वर को समर्पित करने का संकल्प
- गीता के किसी एक श्लोक का मनन
- प्राणायाम और ध्यान का संक्षिप्त अभ्यास
कर्म काल: निष्काम भाव से कर्म
दिन भर के कार्यों में निष्काम भाव को बनाए रखना वैराग्य का व्यावहारिक अभ्यास है। प्रत्येक कार्य को ईश्वर की पूजा मानकर करना चाहिए।
कार्य के दौरान साक्षी भाव का अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए। यह देखना चाहिए कि कौन कार्य कर रहा है और कौन देख रहा है।
दिन भर के अभ्यास:
- हर कार्य से पहले मन में “ईश्वरार्पणम्” कहना
- कार्य के दौरान साक्षी भाव रखना
- सफलता-असफलता में समभाव रखना
- दूसरों के साथ व्यवहार में निस्वार्थ भाव रखना
संध्या काल: दिन भर की समीक्षा
संध्या के समय दिन भर की गतिविधियों की समीक्षा करनी चाहिए। यह देखना चाहिए कि कहाँ आसक्ति हुई और कहाँ वैराग्य रहा।
दिन भर की आसक्तियों का मानसिक त्याग करना चाहिए। यह संकल्प करना चाहिए कि कल और बेहतर तरीके से वैराग्य का अभ्यास किया जाएगा।
संध्याकालीन अभ्यास:
- दिन भर की गतिविधियों का मानसिक जायजा लेना
- जहाँ आसक्ति हुई हो, उसे मानसिक रूप से ईश्वर को समर्पित करना
- कल के लिए वैराग्य का संकल्प दोहराना
- आत्म चिंतन में कुछ समय बिताना
निष्कर्ष: संपूर्ण जीवन में वैराग्य
ईशावास्य उपनिषद का सूत्र “तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः” वैराग्य का सार प्रस्तुत करता है – त्याग करके भोगो। यहाँ त्याग का अर्थ है आसक्ति का त्याग, और भोग का अर्थ है जीवन का पूर्ण आनंद।
वैराग्य जीवन का विरोधी नहीं, बल्कि जीवन को पूर्णता प्रदान करने वाला है। यह न तो अति संसार की सिफारिश करता है और न ही अति त्याग की। यह मध्यम मार्ग है – संसार में रहकर संसार से मुक्त होने का मार्ग।
गृहस्थ धर्म में वैराग्य का अभ्यास करना आधुनिक युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यह मार्ग न केवल व्यक्तिगत मुक्ति का साधन है, बल्कि सामाजिक कल्याण का भी आधार है।
जब गृहस्थ वैराग्य में स्थित हो जाता है, तो वह एक जीवंत उदाहरण बन जाता है। उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणास्रोत बनता है। वह सिद्ध करता है कि आध्यात्मिकता केवल गुफाओं और आश्रमों में ही संभव नहीं, बल्कि घर-परिवार में रहकर भी परम लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है।
अंततः वैराग्य कैवल्य अवस्था तक पहुंचाता है – वह अवस्था जहाँ व्यक्ति अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है। यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है, और यही वेदांत का चरम संदेश है।
गृहस्थ धर्म में वैराग्य का मार्ग कठिन है, परंतु असंभव नहीं। आवश्यकता केवल दृढ़ संकल्प, निरंतर अभ्यास और अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन की है। जो साधक इस मार्ग पर चलने का साहस करता है, वह न केवल अपना कल्याण करता है, बल्कि संपूर्ण समाज के लिए आदर्श बनता है।
मुख्य संदर्भ स्रोत:
- श्रीमद्भगवद्गीता
- ईशावास्य उपनिषद
- कठोपनिषद
- छांदोग्य उपनिषद
- पतंजलि योग सूत्र
- अष्टावक्र गीता
- योग वासिष्ठ
- संत कबीर वाणी
- तुलसीदास रामचरितमानस




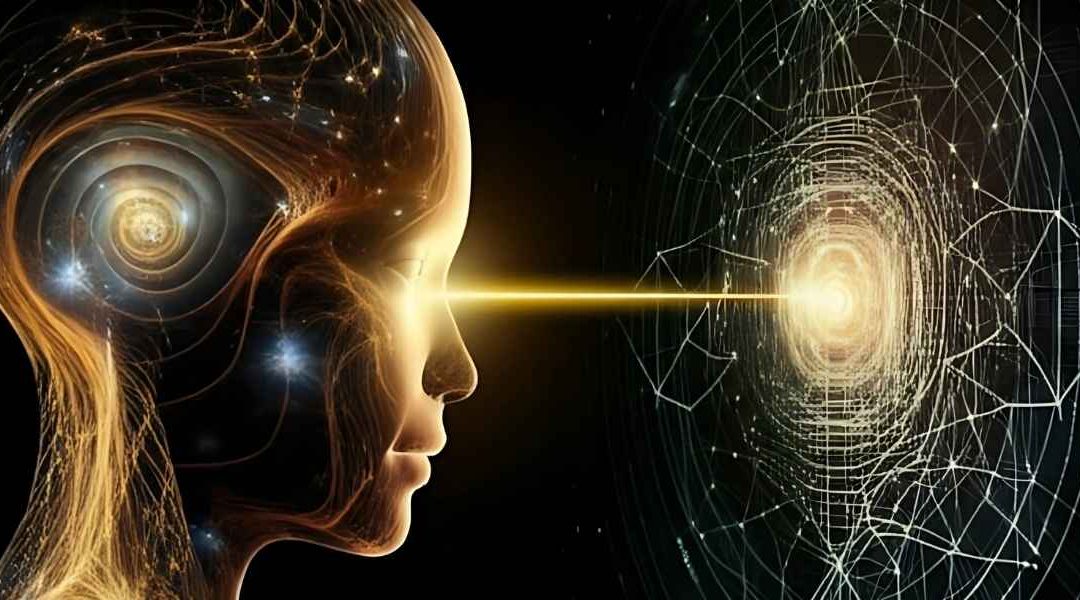

0 Comments