शिव: संसार और सत्य के बीच का सेतु
जब साधक शिव हो जाता है, तब शिव मौन हो जाते हैं
आध्यात्म का महान विरोधाभास
आधुनिक युग में शिव को लेकर जितनी भ्रांतियां हैं, उतनी शायद ही किसी और तत्व को लेकर हों। शिव तो प्रथम गुरु हैं, आदियोगी हैं, समस्त देवत्व से भी परे हैं। पर उपनिषदीय ज्ञान में शिव की जो परिभाषा है, वह इन सबसे कहीं गहरी है। मांडूक्य उपनिषद में स्पष्ट लिखा है – “शिवो हम्” – हम ही शिव हैं।
यह सुनने में जितनी सरल लगती है, अनुभव में उतनी ही जटिल है। क्योंकि शिव केवल पूज्य देवता नहीं, बल्कि संसार और सत्य के बीच एक दिव्य सेतु हैं।
सेतु का प्रारंभिक बिंदु: द्वैत में स्थापना
आम तौर पर आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ द्वैत से होता है। यद्यपि कुछ महान आत्माएं पूर्व स्मृति के साथ जन्म लेती हैं, विशिष्ट कार्य संपन्न करके विलीन हो जाती हैं, तथापि सामान्य साधक के लिए द्वैत ही प्रारंभिक अवस्था है। जिस प्रकार गंगा नदी पर बना कोई सेतु एक किनारे से शुरू होता है, उसी प्रकार शिव पथ भी एक स्पष्ट प्रारंभिक बिंदु रखता है।
कठोपनिषद में नचिकेता की भांति साधक भी मृत्यु के देवता से सत्य जानने की चेष्टा करता है। इस चरण में:
- शिव एक प्राप्त करने योग्य दशा प्रतीत होते हैं
- एक ध्यान करने योग्य स्वरूप लगते हैं
- एक अनुभव करने योग्य चेतना मालूम पड़ते हैं
तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है – “भयउ न कारन अकारन नाहीं। रामकृपा बिन सुलभ न काहीं।” यही द्वैत भाव की शुरुआती अवस्था है जहां कृपा करने वाला अलग है और कृपा पाने वाला अलग।
सेतु का मध्य बिंदु: भाव और रस की अनुभूति
यात्रा के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर साधक को एक अनूठा अनुभव होता है। जब शुद्ध भावना जगती है, तब शिव भाव का ऐसा आनंद मिलता है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता।
एक शिव भक्त के रूप में यह अनुभव:
यहां साधक सोचता है कि बस इसी भाव में बैठे रहना चाहिए। यह शिव रस इतना मधुर होता है कि मन करता है कि इससे कभी आगे न बढ़ना पड़े। पूर्ण द्वैत में आकर, शिव को भगवान मानकर, उनसे प्रेम करते रहना – यही जीवन का चरम सुख लगता है।
पर यहीं ज्ञान मार्गी कहते हैं कि यह भी एक अनुभव है। और यह सत्य भी है। लेकिन यह केवल शुष्क अनुभव नहीं, शिव रस भी है। शिव का प्रत्यक्ष स्वाद है। यदि शिव स्वयं में ज्ञान और आनंद दोनों हैं, तो यह रस स्वयं शिव चेतना से आता है।
यहां महान संतों में भी विविधता दिखती है। मीराबाई कहती हैं – “मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दरद न जाणे कोय।” वहीं कबीर दास कहते हैं – “कबीरा जब हम पैदा नहीं, तब काहे का सुख दुख।”
मीरा सगुण भक्ति मार्ग की थीं और कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। दोनों ही भक्ति के मार्ग पर थे लेकिन अलग-अलग दृष्टिकोण से। इसीलिए दोनों की विचारधारा में भिन्नता होना स्वाभाविक है। दोनों ने अपने सत्य की व्याख्या वैसी की है जैसा उन्होंने देखा। इसका यह अर्थ नहीं कि कोई मार्ग किसी से छोटा या बड़ा है। एक ही सत्य को कहने के दो तरीके हैं, लेकिन हम अस्तित्व की दृष्टि से इस सत्य को नही देखते हैं इसलिए दोनों बातें विरोधाभास जैसी लगती हैं।
वास्तविक समझ:
अनुभवी आध्यात्मिक गुरु इस बात से सहमत हैं कि यह मध्य बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण है। वास्तव में यह अनाहत चक्र या चौथी परत है – संसार और सत्य के मध्य में। गुरु के मूल्यांकन के अनुसार साधक यहां सेतु के ठीक बीच में खड़ा होता है। न तो पूर्णतः संसार में है, न पूर्णतः सत्य में।
यह संक्रमण काल है जहां दोनों का स्वाद मिलता है। कुछ लोग यहीं से सत्य तक पहुंच जाते हैं। कुछ गुरुओं के अनुसार यह छोटा रास्ता है, कुछ के अनुसार लंबा। जो भी हो, यह मध्य अवस्था है। इस भाग में यदि समान मार्ग के अच्छे गुरु का आशीर्वाद और छाया मिल जाए तो यात्रा समाप्त होने की काफी प्रबल संभावना होती है। यद्यपि अनंत संभावनाएं हैं, तो यह भी एक संभावना मात्र ही है। लेकिन काफी प्रबल संभावना है।
सेतु का उत्तरार्ध: शिव का स्वयं को विलीन करना
यहीं आध्यात्म का सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। श्रीमद्भागवत गीता में कृष्ण कहते हैं – “सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।” पहले वे अपनी शरण में आने को कहते हैं, फिर सभी धर्मों को त्यागने की बात करते हैं।
शिव के साथ भी यही अद्भुत खेल होता है। पहले वे आपको अपनी तरफ खींचते हैं, फिर जब भक्त पूर्णतः समर्पित हो जाता है, तब वे स्वयं को गायब कर देते हैं।
आदि शंकराचार्य ने इसे सुंदर तरीके से कहा है – “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः।” जब यह अनुभव हो जाता है, तब न शिव रहते हैं, न शंकर रहते हैं। और जब आप आसपास देखते हैं तो संसार भी नहीं होता, केवल आप ही होते हैं।
सेतु का अंतिम बिंदु: जो शेष रह जाता है
जब शिव गायब हो जाते हैं, तब जो बचता है उसे केवल लक्षणों से पहचाना जा सकता है। मांडूक्य उपनिषद में इसे “तुरीय” कहा गया है – जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से परे है।
रमण महर्षि ने इसे सरल भाषा में समझाया था। एक व्यक्ति ने पूछा – “कैसे पता चलेगा कि आत्मसाक्षात्कार हो गया?” रमण ने मुस्कुराकर कहा – “जब आप यह प्रश्न पूछना बंद कर देंगे।”
इस अवस्था की विशेषताएं:
यहां तक की प्रगति कर चुके साधक में निम्नलिखित विशेषताएं दिखने लगती हैं। वैसे तो विशेषताएं अनंत हैं, यहां प्रमुख चार का उल्लेख है:
- निर्विकल्प शांति जो विचारों से परे हो
- सहज आनंद जो कारण रहित हो
- स्वाभाविक करुणा जो प्रयास रहित हो
- निर्मल चेतना जो स्वयं प्रकाशित हो
व्यावहारिक जीवन में रूपांतरण
इस अवस्था का व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से अलग हो जाता है। श्रीमद्भागवत गीता में इसे “योगस्थः कुरु कर्माणि” कहा गया है।
ऐसा व्यक्ति:
- काम करता है पर कर्ता भाव नहीं रखता
- बोलता है पर वक्ता नहीं होता
- देखता है पर द्रष्टा नहीं होता
कबीर दास जी ने इसे खूबसूरत अंदाज में कहा है: “कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर।
न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर।”
समसामयिक प्रासंगिकता
आज के तनावपूर्ण समय में शिव की यह शिक्षा और भी प्रासंगिक हो जाती है। जब चारों तरफ अहंकार की होड़ मची हो, तब शिव का यह संदेश कि अपने अहंकार को ही मिटा दो, एक क्रांतिकारी विचार है।
महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में स्पष्ट लिखा है – “स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारासेवितो दृढभूमिः।” यानी लंबे समय तक, निरंतर और श्रद्धा के साथ अभ्यास करने से ही दृढ़ता आती है।
निष्कर्ष: सेतु का कार्य पूर्ण
अंततः यही है शिव की महानता। वे आध्यात्मिक संसार के सबसे निस्वार्थ गुरु हैं। वे अपने शिष्य को खुद जैसा बनाकर अपने आप को ही मिटा देते हैं।
स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने ठीक ही कहा था – “गुरु वह है जो शिष्य को अपने से भी ऊपर उठा दे।”
जब शिव संसार और सत्य के बीच सेतु का कार्य पूरा कर देते हैं, तब वे स्वयं विलीन हो जाते हैं। फिर कुछ समय में साधक को बोध हो जाता है कि वे शिव स्वयं ही हैं। उस समय न संसार रहता है, न सत्य की कोई अलग सत्ता – केवल एक ही अस्तित्व रह जाता है। और उसी को हम सत्य कह देते हैं।
सत्य में शिव वह अवस्था है जिसका द्वार सांसारिक शिव में मिटने पर खुलता है।
अंतिम सत्य
“जब साधक शिव हो जाता है, तब शिव मौन हो जाते हैं।”
क्योंकि अब बोलने वाला कौन बचा है और सुनने वाला कौन?
संदर्भ ग्रंथ:
- मांडूक्य उपनिषद
- कठोपनिषद
- श्रीमद्भागवत गीता
- योग सूत्र – महर्षि पतंजलि
- रामचरितमानस – तुलसीदास
- स्वामी विवेकानंद के व्याख्यान
- रमण महर्षि के संवाद




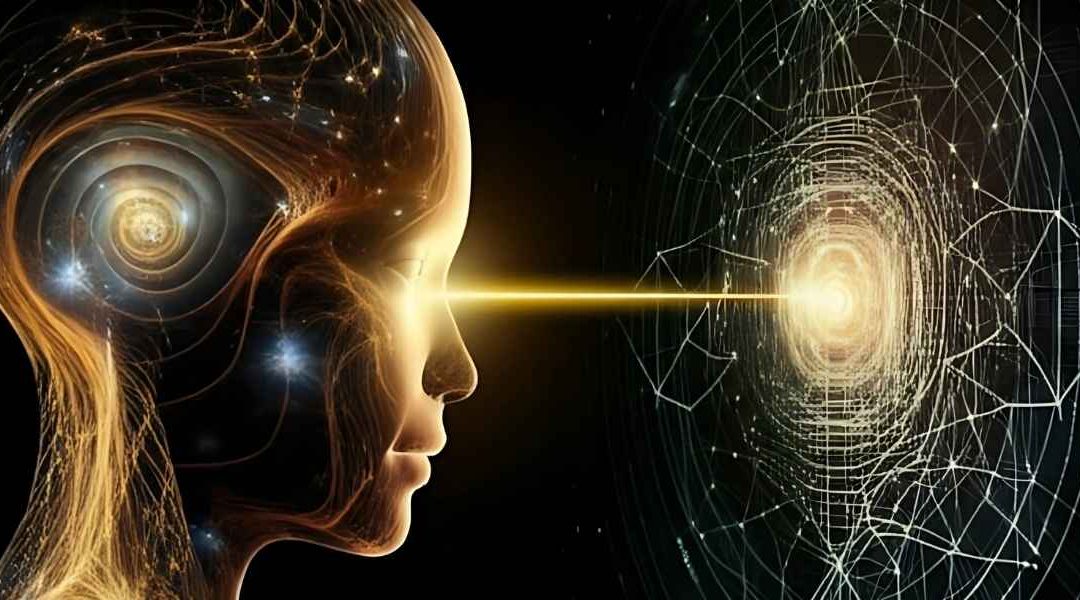

0 Comments