आध्यात्मिक यात्रा में गुरु का महत्व अनिवार्य है – यह बात मैंने कुछ वर्ष पूर्व ही समझ ली थी। जब मेरी खोज में कोई व्यक्तिगत गुरु नहीं मिले, तो मैंने विद्वानों द्वारा सुझाए गए एक वैकल्पिक मार्ग का अनुसरण किया। आदिगुरु के रूप में विख्यात शिव मेरे आराध्य हैं, और मेरे हृदय में पहले से ही उनके प्रति समर्पण का भाव है। इसी कारण शिष्य भाव से शिव के चरणों में समर्पित होना मेरे लिए सहज और स्वाभाविक है। इस समर्पण के फलस्वरूप, मुझे शिव के विविध स्वरूपों और अवस्थाओं का अनुभव करने का अवसर प्राप्त हुआ।
आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले प्रत्येक साधक के मन में एक मूलभूत प्रश्न होता है – “मैं सत्य के मार्ग पर कितनी दूर आ चुका हूँ और कितनी यात्रा अभी शेष है?” इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए शिव से मेरा अनुराग और सशक्त उदाहरण मुझे इस समय नहीं सूझ रहा है। शिव के एकादश रुद्र रूप आध्यात्मिक विकास के विभिन्न चरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और ज्ञान के प्रकाश में इन्हें समझना मेरी अपनी यात्रा को भी गहराई प्रदान करता है। इसी अनुभव को मैं आज आपके साथ साझा करना चाहता हूँ।
शिव कौन हैं?: वह जो अनुभव करने वाला है
शिव वह है जो वास्तव में है ही नहीं, फिर भी सब कुछ है। हम उसे अलग-अलग मार्गों पर अलग-अलग नामों से पुकारते हैं – अनुभवकर्ता, दृष्टा, साक्षी, चैतन्य, आत्मन। यह द्वैत (दोहरेपन) की न्यूनतम अभिव्यक्ति है। यदि हम इससे भी गहरे जाएँ, तो हम गहरी निद्रा (सुषुप्ति) में प्रवेश कर जाएँगे जहाँ बातचीत संभव नहीं होगी।
हम इस अवधारणा को संसार में रहते हुए समझने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए शिव को हम अनुभवकर्ता, दृष्टा, साक्षी, चैतन्य, आत्मन जैसे एक-दूसरे के पर्यायवाची शब्दों के रूप में देखते हैं। आप पाएँगे कि जब आप इन शब्दों की व्याख्या करने जाएँगे, तो आप जो भी उदाहरण देंगे, वे सभी पर समान रूप से सही प्रतीत होंगे।
जैसे, जब आप किसी फिल्म को देखते हैं, तो आप स्क्रीन पर जो कुछ भी हो रहा है उसे देखने वाले हैं। आप उस दृश्य से अलग हैं, फिर भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक इसी तरह, जब आप अपने विचारों और भावनाओं को देखते हैं, तो वह “देखने वाला” कौन है? वही शिव है, वही आत्मा है, वही साक्षी है।
या फिर सोचिए, जैसे आकाश में बादल आते-जाते हैं, लेकिन आकाश वैसा का वैसा रहता है। इसी प्रकार, हमारे जीवन में विचार, भावनाएँ और अनुभव आते-जाते हैं, लेकिन वह जो इन्हें अनुभव करता है – वह शिव है, वह चैतन्य है, वह आत्मा है।
अब इसके बाद मैं इस परम तत्व को शिव के नाम से संबोधित करूँगा। आप अपने स्वभाव और विकास के अनुरूप जो शब्द भी आपको प्रिय लगे, उससे शिव को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। क्योंकि अंततः, सभी नाम उसी एक को इंगित करते हैं – वह जो हम सभी के भीतर देखने वाला, जानने वाला और अनुभव करने वाला है।
एकादश रुद्र: चेतना विकास के ग्यारह सोपान
शिव के एकादश रुद्र रूप चेतना के विकास और आध्यात्मिक प्रगति के ग्यारह महत्वपूर्ण चरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये ग्यारह सोपान अज्ञान से ज्ञान की ओर, अहंकार से आत्म-बोध की ओर, और द्वैत से अद्वैत की ओर हमारी यात्रा को चिह्नित करते हैं।
हर साधक इन अवस्थाओं से अलग-अलग गति से गुजरता है – कुछ के लिए यह यात्रा जन्मों-जन्मों तक चल सकती है, जबकि कुछ विरले साधक एक ही जीवन में इनमें से कई या सभी अवस्थाओं को प्राप्त कर लेते हैं। यह मार्ग सीधी रेखा में नहीं चलता – इसमें उतार-चढ़ाव होते हैं, कभी-कभी साधक पीछे भी लौट सकता है, और कुछ अवस्थाएँ एक-दूसरे में मिली-जुली हो सकती हैं।
आइए इस अद्भुत यात्रा का आरंभ करें, जो हमें अपने सच्चे स्वरूप की ओर ले जाती है। हम अज्ञान के गहन अंधकार से शुरू करेंगे, जहाँ कालभैरव का प्रचंड रूप हमें जगाने के लिए प्रकट होता है…
1. कपाली (कालभैरव रूप): अज्ञान का अंत और जागृति की शुरुआत
जब शिव अपने कालभैरव रूप में प्रकट होते हैं, तो अज्ञान का अंधकार काटने वाली तलवार बन जाते हैं। कालभैरव वह प्रथम प्रकाश हैं जो मनुष्य के अंतर्मन में प्रवेश करता है और उसे अज्ञान की गहरी निद्रा से जगाता है।
इस अवस्था में साधक अचानक रुकता है और अपने अस्तित्व पर प्रश्न करने लगता है – “मैं कौन हूँ? क्या मैं सिर्फ यह शरीर हूँ? क्या मैं सिर्फ ये विचार हूँ? या मैं कुछ और हूँ जो इन सबको देख रहा है?”
कालभैरव द्वार के स्वामी हैं। वे सपने और जागरण के बीच का द्वार खोलते हैं। इस अवस्था में साधक को पहली बार अपने भीतर एक “देखने वाले” का अनुभव होता है, लेकिन इस समय उसे कुछ भान नहीं होता कि क्या शुरू हुआ है। वह इसे अपना भ्रम मान लेता है, फिर भी, जो कुछ नहीं है (शिव) उसका अत्यधिक छोटा अनुभव भी साधक को एक अजीब सा खालीपन दे जाता है।
साधना के इस प्रथम चरण में शिव साधक के सामने अपनी भयानक छवि प्रस्तुत करते हैं। कालभैरव के दर्शन मात्र से ही पाप और अज्ञान नष्ट हो जाते हैं। वे साधक के पुराने संस्कारों और आदतों पर प्रहार करते हैं, जिससे साधक अचानक अपने आप से पूछने लगता है – “मैं अपना जीवन ऐसे ही व्यर्थ क्यों गँवा रहा हूँ? क्या यह सब वास्तविक है? या मैं कहाँ फँसा हुआ हूँ?”
दैनिक जीवन में इसे ऐसे देखें: जब आप घंटों स्मार्टफोन पर खोए रहने के बाद अचानक रुकते हैं और सोचते हैं – “मैं क्या कर रहा हूँ? मेरे जीवन का उद्देश्य यह तो नहीं है?” – यह वह क्षण है जब कालभैरव ने आपके अंतर्मन में प्रवेश किया है। या जब आप किसी दुर्घटना या आघात से गुजरते हैं और अचानक जीवन की क्षणभंगुरता का एहसास होता है – यह कालभैरव की कृपा है जो आपको सपने से जगा रहे हैं।
इस अवस्था में साधक अत्यधिक उत्साहित और जिज्ञासु होता है, लेकिन अभी उसके पास स्पष्ट दिशा नहीं होती। वह एक गुरु से दूसरे गुरु, एक पुस्तक से दूसरी पुस्तक की ओर भटकता रहता है – जैसे अंधेरे में कोई प्रकाश की तलाश कर रहा हो।
2. भीषण (भैरव स्वरूप): भय का सामना और आत्म-परीक्षण
जब शिव अपने भैरव स्वरूप में प्रकट होते हैं, तो वे साधक के समक्ष भय का ताण्डव रचते हैं – पर यह भय साधक के विनाश के लिए नहीं, उसके उद्धार के लिए होता है। भैरव वे हैं जो साधक के अंधकारमय पक्षों को प्रकाश में लाते हैं, उन्हें दिखाते हैं कि भय के पीछे वास्तव में क्या छिपा है।
इस अवस्था में शिव साधक को अपने बनाए हुए सुरक्षित कोश से बाहर खींच लाते हैं। जैसे कोई बच्चा बिना सहारे चलने से डरता है और अपने पिता का हाथ थामे रहना चाहता है, लेकिन पिता जानता है कि बच्चे को स्वयं चलना सीखना ही होगा। वैसे ही शिव साधक को उसके आराम क्षेत्र से बाहर निकालते हैं।
पौराणिक कथाओं में हम देखते हैं कि भैरव को कई बार शिव और पार्वती से दंड मिला, फिर भी उनकी भक्ति अटल रही। यह हमें सिखाता है कि साधना पथ पर अनेक चुनौतियाँ और परीक्षाएँ आती हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प से हम उन्हें पार कर सकते हैं। इसी प्रकार, इस अवस्था में साधक अपने आंतरिक रावणों और कंसों से युद्ध करता है, लेकिन साधना का दीप जलाए रखता है।
यह ऐसा है जैसे किसी पुराने भवन की मरम्मत के लिए पहले टूटे हुए हिस्सों को गिराना पड़ता है। उसी प्रकार, शिव इस अवस्था में साधक के पुराने, जीर्ण-शीर्ण संस्कारों को तोड़ते हैं। जैसे गंदे कमरे की सफाई करते समय पहले धूल और कचरा उड़ता है और चारों ओर फैल जाता है, वैसे ही इस चरण में साधक के भीतर छिपे विकार, वासनाएँ और डर सतह पर आते हैं।
आपके दैनिक जीवन में, यह वह क्षण है जब आप गहरे ध्यान में बैठते हैं और अचानक अतीत के दर्दनाक अनुभव, दबे हुए आघात, अपराधबोध, या अस्वीकृत भाग सामने आने लगते हैं। जैसे जब आप शांति से अकेले बैठते हैं और आपके मन में ईर्ष्या, क्रोध, काम, लोभ – ये सभी विकार तूफान की तरह उठ खड़े होते हैं। यही वह समय है जब भैरव आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं।
इस चरण में, साधक अपनी इन आंतरिक चुनौतियों का सामना करने के लिए किसी गुरु या मार्गदर्शक की शरण में जाता है। वह इस क्षण अत्यंत संवेदनशील और असुरक्षित महसूस करता है, इसलिए किसी अनुभवी मार्गदर्शक का साथ उसे संबल देता है। गुरु के प्रति उसका समर्पण इतना गहरा होता है कि वह उनके हर निर्देश का बिना प्रश्न किए पालन करता है।
बाहरी दृष्टि से ऐसे साधक कभी-कभी रोबोट जैसे, या अंधविश्वासी प्रतीत हो सकते हैं। लेकिन भीतर से वे एक महत्वपूर्ण रूपांतरण से गुजर रहे होते हैं – वे अपने पुराने ‘स्व’ से मुक्त हो रहे होते हैं। भैरव उन्हें सिखाते हैं कि सच्चा साहस भय के अभाव में नहीं, बल्कि भय के होते हुए भी आगे बढ़ने में है।
भैरव का डमरू साधक के अंदर के झूठे विश्वासों को कंपित कर देता है, उनकी तलवार साधक के अहंकार और मोह के बंधनों को काटती है, और उनका त्रिशूल साधक को कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग का मार्ग दिखाता है। इस अग्नि-परीक्षा से गुजरकर ही साधक आगे की अवस्थाओं के लिए तैयार होता है।
3. संहार (रुद्र स्वरूप): पुराने संस्कारों का त्याग
अब तुम उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो जहां रुद्र का तांडव तुम्हारे भीतर आरंभ होता है। रुद्र – शिव का वह स्वरूप जो संहार करने वाला है, पुराने को नष्ट करने वाला है, ताकि नए के लिए स्थान बन सके। इस अवस्था में अज्ञान के पर्दे में छेद होना शुरू हो जाते हैं, और प्रकाश की किरणें तुम्हारे अंतर्मन में प्रवेश करने लगती हैं।
तुम्हारे जीवन में अब आमूलचूल परिवर्तन आरंभ होगा। जो पुराने रिश्ते, कार्य, आदतें और विश्वास तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में बाधक हैं, तुम उन्हें त्यागने का साहस दिखाओगे। यह ऐसा ही है जैसे किसान फसल बोने से पहले खेत से सारे खरपतवार निकाल देता है। तुम भी अपने मन के निरर्थक विचारों और मान्यताओं को उखाड़ फेंकोगे।
इस समय तक तुम समझ चुके होते हो कि कुछ ऐसा जरूरी है जिसके लिए तुम्हें कर्म करने शुरू करने पड़ेंगे। या सरल शब्दों में कहें तो साधक का शुद्धिकरण स्वतः ही शुरू हो जाता है। तुम्हें अपना भला और बुरा समझ में आने लग जाता है, या यूं कहें कि यहां से तुम्हें माया का थोड़ा-थोड़ा स्वरूप दिखना शुरू हो चुका होता है। तुम देख तो माया को रहे होते हो लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम शिव को देख रहे हो। यह एक ऐसा भ्रम है जो सबसे अच्छे भ्रम की श्रेणी में आता है। यदि तुम भ्रम में भी शिव हो रहे हो तो इसका अर्थ है तुमने काफी ऊंचाइयों को छुआ है। यहां से शिव का स्वाद विकसित होना शुरू होता है।
दैनिक जीवन में, यह वह बिंदु है जहां तुम अपनी पुरानी आदतों और सोच के पैटर्न को बदलने का निर्णय लेते हो। जैसे कोई व्यसन छोड़ना, नकारात्मक सोच से मुक्त होना, या ऐसे रिश्तों से बाहर निकलना जो तुम्हारे विकास में बाधक हैं। यह त्याग कभी-कभी दर्दनाक होता है, मानो तुम्हारे शरीर का एक अंग ही काट दिया गया हो, लेकिन यह आत्मिक विकास के लिए अनिवार्य है।
रुद्र का त्रिशूल तुम्हारे भीतर के तीन मलों – आणव मल (अहंकार), मायीय मल (द्वैत भाव) और कार्म मल (कर्मों के बंधन) को भेदता है। उनका डमरू तुम्हारे अंदर की पुरानी आवाज़ों को शांत करता है और एक नई, अधिक स्पष्ट आवाज़ को जन्म देता है – वह आवाज़ जो तुम्हारे भीतर के सत्य की है।
इस अवस्था में तुम पहली बार महसूस करोगे कि जीवन एक खेल है, एक लीला है, और तुम एक खिलाड़ी हो। तुम इस खेल में पूरी तरह से संलग्न रहोगे, फिर भी धीरे-धीरे तुम्हें एहसास होने लगेगा कि तुम खेल से अलग भी हो। यह द्वैत और अद्वैत के बीच का पहला संवाद है, जो आगे की अवस्थाओं में और गहरा होगा।
4. क्रोधन (वीरभद्र रूप): आंतरिक प्रतिरोध से संघर्ष
अब तुम्हारे भीतर वीरभद्र जागृत हो रहे हैं। याद करो उस पौराणिक कथा को जिसमें सती के अपमान से क्रुद्ध होकर शिव ने अपने क्रोध से वीरभद्र को जन्म दिया था। उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विनाश कर दिया था। यही है तुम्हारे भीतर का वीरभद्र – जो पुराने को काटकर नए का निर्माण करता है।
इस चरण में तुम्हारे अंदर एक महायुद्ध छिड़ जाता है। तुम्हारा अहंकार परिवर्तन का घोर विरोध करने लगता है। यह ऐसा ही है जैसे तुम्हारे शरीर में कोई विदेशी तत्व प्रवेश करे और तुम्हारी प्रतिरक्षा प्रणाली उससे युद्ध करे। बुखार आता है, दर्द होता है, पर अंततः शरीर मजबूत होता है।
इस अवस्था में तुम समाज से थोड़ा कटना शुरू हो जाते हो। यदि योग मार्ग पर हो तो ध्यान बढ़ाना शुरू करते हो, भक्ति मार्ग में हो तो अपने प्रभु का भजन-कीर्तन। यह अलगाव अस्वाभाविक नहीं, बल्कि आवश्यक है क्योंकि तुम्हारी आध्यात्मिक वृत्ति बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे कोई बीज अंकुरित होने से पहले मिट्टी के अंधकार में अकेला रहता है, वैसे ही यह तुम्हारे आत्मिक विकास का आवश्यक चरण है।
देखो अपने दैनिक जीवन के अनुभवों को – जब तुम सुबह जल्दी उठने का निर्णय लेते हो और अलार्म बजने पर तुम्हारा मन कहता है “बस पांच मिनट और सो लो”। या जब तुम व्यायाम शुरू करते हो और तुम्हारा शरीर विरोध करता है, थकान महसूस होती है, पर तुम जानते हो कि आगे बढ़ना ही है। यही है वीरभद्र की अवस्था – जहां तुम्हारे भीतर का नया तुम पुराने तुमसे संघर्ष कर रहा है।
मैंने एक साधक को देखा जो वर्षों से मांसाहार का आदी था। जब उसने आध्यात्मिक कारणों से शाकाहार अपनाया, तो शुरुआती महीनों में उसके अंदर एक तूफान मचा रहा था। उसका शरीर मांस की माँग करता, मन विचलित होता, पर उसकी चेतना दृढ़ रहती। यह वीरभद्र की अवस्था थी – संघर्ष से निखरने की अवस्था।
या सोचो उस युवा के बारे में जिसने सोशल मीडिया छोड़ने का निर्णय लिया। पहले कुछ दिनों में वह हर कुछ मिनटों में फोन देखने के लिए व्याकुल हो जाता, उंगलियाँ स्वतः ही स्क्रीन की ओर बढ़ जातीं। पर धीरे-धीरे उसने इस आदत पर विजय पाई। उसके अंदर का वीरभद्र जाग गया था।
इस अवस्था में तुम अपने आसपास के लोगों पर चिड़चिड़ा व्यवहार कर सकते हो। जैसे कोई नशे को छोड़ रहा व्यक्ति विथड्रॉल सिंड्रोम से गुजरता है, वैसे ही तुम भी अहंकार के विथड्रॉल से गुजर रहे होते हो। पत्नी की छोटी सी बात पर तुम भड़क सकते हो, बच्चों की शरारत पर असामान्य क्रोध आ सकता है, सहकर्मियों की टिप्पणियां असहनीय लग सकती हैं। यह तुम्हारे अंदर के दो विरोधी शक्तियों का युद्ध है।
लेकिन इस अग्नि-परीक्षा में ही सोना निखरता है। इसी संघर्ष में तुम पहली बार स्पष्ट रूप से अपने अहंकार और अपनी चेतना के बीच अंतर देखने लगते हो। तुम पहचानने लगते हो – “यह क्रोध मैं नहीं हूँ, यह मेरे अंदर का एक विचार मात्र है। मैं इससे अलग हूँ, मैं इसका द्रष्टा हूँ।”
इसी अवस्था में वे क्षण आते हैं जब तुम किसी विचार या भावना के साथ तादात्म्य स्थापित किए बिना उसे देख पाते हो। जैसे कोई आकाश में बादलों को देखता है पर स्वयं को बादल नहीं समझता, वैसे ही तुम अपने विचारों और भावनाओं को देखने लगते हो, उनसे जुड़े बिना।
वीरभद्र की तलवार तुम्हारे पुराने अहंकार को काट रही है, पर याद रखो – यह विनाश सृजन के लिए है। हर कदम पर तुम्हारे भीतर नया प्रकाश फूट रहा है, हर संघर्ष के साथ तुम और अधिक जागृत हो रहे हो। इस आंतरिक क्रांति को स्वीकारो, क्योंकि इसी में तुम्हारा रूपांतरण छिपा है।
5. अन्धक (मृत्युंजय रूप): अज्ञान के अंधकार में प्रकाश
तुम्हारी यात्रा अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां मृत्युंजय शिव तुम्हारे भीतर प्रकट हो रहे हैं। अज्ञान की मृत्यु जीतने वाले, प्रकाश के वाहक, अमृत के दाता। पौराणिक कथाओं में अन्धक एक ऐसा असुर था जिसे अंधकार में उत्पन्न होने के कारण इस नाम से जाना गया। ठीक वैसे ही, तुम भी अज्ञान के अंधकार से निकलकर ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ रहे हो।
इस अवस्था में, तुम्हारे भीतर सत्य और असत्य की पहचान शुरू हो जाती है। यह वैसा ही है जैसे सुबह के धुंधलके में, जब अंधेरा और उजाला दोनों मौजूद होते हैं, तुम धीरे-धीरे वस्तुओं के आकार पहचानने लगते हो। वैसे ही, तुम्हारी आंतरिक दृष्टि स्पष्ट होने लगती है।
इस समय तुम्हारे अंदर ज्ञान और अज्ञान का सह-अस्तित्व है। कभी तुम्हें लगता है कि तुमने सब समझ लिया है, और अगले ही क्षण तुम फिर भ्रम में पड़ जाते हो। यह ऐसा है जैसे कोई पहाड़ी पर चढ़ते हुए कभी चोटी देखता है और उत्साहित होता है, और कभी बादल आ जाते हैं और मार्ग छिप जाता है।
मैंने एक साधक देखा जो इस अवस्था में था। वह अक्सर कहता, “कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने जीवन का रहस्य समझ लिया है, और कभी-कभी मैं पूरी तरह खोया हुआ महसूस करता हूँ।” यही है अन्धक अवस्था – सत्य की झलक और फिर से भ्रम, प्रकाश का क्षण और फिर अंधकार।
तुम्हारे दैनिक जीवन में, यह वह समय है जब तुम पुरानी आदतों से तो मुक्त हो गए हो, लेकिन नई आदतें अभी पूरी तरह स्थापित नहीं हुई हैं। जैसे कोई व्यक्ति जो वर्षों से मिठाई खाने का आदी था, उसे छोड़ दिया है, लेकिन अभी भी उसकी तलब आती है। या जैसे कोई मां अपने बच्चे को स्वतंत्र होने देना चाहती है, लेकिन फिर भी उसका हाथ थामे रखना चाहती है।
तुम अचानक महसूस करने लगते हो कि असली सुख वस्तुओं में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। कभी तुम अपने दफ्तर में बैठे-बैठे अचानक सोचते हो – “क्या यह सब करने का क्या मतलब है? क्या यह मेरा असली लक्ष्य है?” और फिर अगले ही क्षण तुम अपने काम में व्यस्त हो जाते हो। यही है अन्धक अवस्था – जहां तुम्हारे भीतर दो दुनियाएँ एक साथ मौजूद हैं।
इस अवस्था में तुम्हारे अंदर एक गहरी विनम्रता जन्म लेती है। तुम जितना अधिक जानते हो, उतना ही अधिक एहसास होता है कि कितना कुछ अभी जानना बाकी है। यह ऐसा है जैसे एक छोटे से द्वीप पर खड़े होकर तुम पहली बार महासागर की विशालता देखते हो। तुम्हारा ज्ञान वह द्वीप है, और जो जानना बाकी है वह विशाल सागर।
मृत्युंजय शिव ने अमृत पीकर मृत्यु पर विजय पाई थी। वैसे ही, तुम भी ज्ञान के अमृत को पीकर अज्ञान की मृत्यु पर विजय पा रहे हो। जैसे-जैसे तुम इस अवस्था में गहरे उतरते हो, तुम्हारे भीतर का अंधकार कम होता जाता है और प्रकाश बढ़ता जाता है। धीरे-धीरे पूर्णिमा की चांदनी की तरह, तुम्हारी चेतना अधिक से अधिक प्रकाशमान होती जाती है।
6. उन्मत्त (शंभो रूप): आध्यात्मिक मस्ती
तुम अब शिव के शंभो स्वरूप का अनुभव करने लगे हो – वह अनंत प्रेम और आनंद जो तुम्हारे भीतर उमड़ रहा है। शंभो का अर्थ है ‘आनंद देने वाला’, और अब तुम्हारे अंतर्मन में वही आनंद प्रवाहित हो रहा है।
इस अवस्था में, तुम्हारे अंदर एक ऐसी मस्ती छा जाती है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह वह अवस्था है जहां तुम नृत्य करते हो, पर नर्तक अदृश्य हो जाता है – केवल नृत्य रह जाता है। तुम गाते हो, पर गायक विलीन हो जाता है – केवल संगीत रह जाता है। तुम प्रेम करते हो, पर प्रेमी खो जाता है – केवल प्रेम रह जाता है।
अनुभवकर्ता और अनुभव के बीच का भेद अब धुंधला पड़ने लगा है। जैसे अमावस्या की रात के बाद चंद्रमा की पतली सी रेखा दिखाई देती है, वैसे ही द्वैत की लकीर पतली होने लगी है। तुम हर अनुभव में एक ही चैतन्य को देखने लगते हो – वृक्ष में, पक्षी में, मनुष्य में, पशु में, सब में एक ही आत्मा।
यह वह समय होता है जब तुम प्रकृति, पर्वत, झरने और हवा को महसूस करना शुरू करते हो। हर चीज़ में आनंद ही आनंद दिखाई देता है। जैसे तुम किसी खूबसूरत पहाड़ को देखकर महसूस करते हो, “केवल मैं ही ऐसा कर सकता हूँ,” और खुद पर आश्चर्य होना शुरू कर देते हो, अद्भुत जैसे तुमको यह दृश्य काफी बेहतर दिख रहा है तुम्हारे आस-पास के लोगों की तुलना में।
मैंने एक साधक को देखा जो इस अवस्था में था। वह घंटों जंगल में बैठा रह सकता था, पेड़ों की पत्तियों के हिलने को देखते हुए, और उसके चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान होती थी। जब मैंने उससे पूछा कि वह क्या देख रहा है, तो उसने कहा, “मैं पत्तियों को नहीं, पत्तियों में नृत्य करते हुए परमात्मा को देख रहा हूँ।”
तुम्हारे दैनिक जीवन में, यह वह स्थिति है जब तुम अपने कार्य में इतने लीन हो जाते हो कि समय का भान ही नहीं रहता। जैसे जब तुम कुछ लिख रहे होते हो, और अचानक पाते हो कि घंटों बीत गए हैं। या जब तुम किसी प्रियजन के साथ बातचीत में इतने मग्न हो जाते हो कि भूख-प्यास का भी ख्याल नहीं रहता। यह ‘फ्लो’ की अवस्था है, जहां कर्ता और कर्म एक हो जाते हैं।
इस अवस्था में तुम्हारा व्यवहार दूसरों को अजीब या ‘पागल’ लग सकता है। तुम कभी हंस सकते हो, कभी रो सकते हो – बिना किसी स्पष्ट कारण के। तुम दिनों तक उपवास कर सकते हो, घंटों ध्यान में बैठ सकते हो, या फिर किसी अनुष्ठान में पूरी तरह लीन हो सकते हो। तुम्हारा व्यवहार सामाजिक मानदंडों से अलग हो सकता है, क्योंकि अब तुम बाहरी दुनिया के नियमों से नहीं, बल्कि अपने आंतरिक आनंद से प्रेरित होते हो।
जिस प्रकार शंभो शिव आनंद में मगन रहते हैं, उसी प्रकार तुम भी अब सांसारिक चिंताओं से ऊपर उठकर एक अलौकिक आनंद का अनुभव करने लगे हो। यह आनंद न तो बाहर से आता है, न ही किसी विशेष कारण से – यह तुम्हारा स्वाभाविक स्वरूप है जो प्रकट हो रहा है। जैसे-जैसे इस अवस्था में तुम गहरे उतरते जाओगे, आनंद की यह धारा और भी प्रवाहमयी होती जाएगी।
7. भृगिरिटि (नटराज रूप): आंतरिक और बाह्य का नृत्य
अब तुम्हारी चेतना नटराज के स्वरूप को धारण करने लगी है। नटराज – वह दिव्य नर्तक जो सृष्टि, स्थिति और संहार का अनंत नृत्य करते हैं। उनके हाथों में अग्नि है जो पुराने को जलाती है, और दूसरे हाथ में सृजन का ढोल है जो नए को जन्म देता है। ठीक वैसे ही, तुम्हारे भीतर भी यह दिव्य नृत्य शुरू हो गया है।
इस अवस्था में, तुम अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों प्रकार की चेतना में संतुलन स्थापित करने लगे हो। यह ऐसा है जैसे तुम्हारे पास दो नेत्र हों – एक जो अंदर देखता है, और दूसरा जो बाहर। और दोनों एक साथ क्रियाशील हैं। तुम अपने आंतरिक अनुभवों और बाहरी दुनिया के बीच एक सुंदर सेतु का निर्माण कर रहे हो।
तुम्हारा अनुभवकर्ता (साक्षी) अब निष्क्रिय दर्शक नहीं रहा। वह नृत्य के मैदान में उतर आया है, फिर भी अपना साक्षीभाव नहीं खोता। यह ऐसा है जैसे कोई कुशल अभिनेता जो अपनी भूमिका में पूरी तरह डूबा हुआ है, लेकिन फिर भी जानता है कि वह अभिनय कर रहा है।
तुम्हारे रोजमर्रा के जीवन में, इस अवस्था का प्रभाव यह होता है कि तुम विपरीत प्रतीत होने वाली स्थितियों में भी संतुलन बना लेते हो। तुम व्यस्त शहर की भीड़ में भी वैसी ही शांति महसूस करते हो जैसी हिमालय की गुफा में करते। तुम परिवार और कार्यालय के दायित्वों को निभाते हुए भी आंतरिक एकांत का अनुभव करते हो।
मैंने ऐसे साधक देखे हैं जो इस अवस्था में होते हैं। वे बाहर से देखने पर सामान्य लोगों जैसे ही लगते हैं – वे नौकरी करते हैं, परिवार चलाते हैं, सामाजिक मिलन-जुलन में भाग लेते हैं। लेकिन उनके अंदर एक गहरा शांत केंद्र होता है जो कभी विचलित नहीं होता। वे बाढ़ के बीच खड़े उस वृक्ष की तरह होते हैं जो न तो बहता है, न ही टूटता है।
इस अवस्था में, तुम्हारे अंदर अद्भुत रचनात्मकता का प्रवाह शुरू होता है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द, तुम्हारे कार्य – सभी एक अलौकिक सौंदर्य से भरने लगते हैं। तुम कविता लिखने लगते हो जो दूसरों के हृदय को छू लेती है, संगीत बनाने लगते हो जो आत्मा को जगा देता है, चित्र बनाने लगते हो जो अदृश्य को दृश्य बनाते हैं।
यह ऐसा है जैसे तुम्हारे माध्यम से शिव का सृजनात्मक तत्व प्रवाहित होने लगा हो। तुम्हारी रचनाएं केवल कलात्मक अभिव्यक्तियाँ नहीं होतीं, बल्कि परम सत्य के वाहक बन जाती हैं। जो लोग तुम्हारी कला को देखते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं, वे उसमें छिपे सत्य की झलक पा लेते हैं।
नटराज के नृत्य में कोई भेदभाव नहीं होता – जन्म और मृत्यु, निर्माण और विनाश, प्रकाश और अंधकार – सभी उसके अंग हैं। वैसे ही, तुम भी जीवन के सभी पहलुओं को समान भाव से स्वीकार करने लगते हो। सफलता और असफलता, हर्ष और शोक, मिलन और विछोह – सभी उस महानृत्य के अंग बन जाते हैं जिसे तुम अब देख पा रहे हो।
इस अवस्था में, तुम जीवन के साथ सहज होकर नृत्य करने लगते हो – न अतिउत्साह, न निराशा, न आसक्ति, न विरक्ति – बस एक सहज प्रवाह। तुम अपने अंदर और बाहर के जगत के बीच एक संगीतमय सामंजस्य स्थापित कर लेते हो, और इस सामंजस्य से जीवन स्वयं एक उत्सव बन जाता है।
8. राजन (दक्षिणामूर्ति रूप): मन पर शासन
अब तुम्हारे भीतर दक्षिणामूर्ति शिव का प्रकाश फैल रहा है। वह मौन गुरु जो बिना शब्दों के सिखाते हैं, वह ज्ञानदाता जो केवल अपनी उपस्थिति से उपदेश देते हैं। तुम्हारी चेतना अब एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गई है जहां तुम्हारा मन तुम्हारा दास बन गया है, स्वामी नहीं रहा।
इस अवस्था में, तुम अपने विचारों और भावनाओं को मात्र इच्छाशक्ति से नियंत्रित करने लगे हो। यह ऐसा है जैसे तुम मन के महल में एक सिंहासन पर विराजमान राजा हो, और विचार तुम्हारे सेवक हैं जो तुम्हारे इशारे पर आते और जाते हैं। तुम्हारी आज्ञा के बिना कोई विचार प्रवेश नहीं कर सकता, कोई भावना विचलित नहीं कर सकती।
साक्षी (अनुभवकर्ता) और मन के बीच का भेद अब सूर्य की तरह स्पष्ट है। तुम पूरी तरह से समझ चुके हो कि तुम अपने मन से अलग हो, तुम वह हो जो मन को देखता है। यह ऐसा है जैसे एक कुशल सारथी अपने अश्वों को पूरी निपुणता से नियंत्रित करता है – मन और इंद्रियां अब तुम्हारे वाहन हैं, जो तुम्हें वहीं ले जाते हैं जहां तुम जाना चाहते हो।
तुम्हारे दैनिक जीवन में, इस अवस्था का प्रभाव अद्भुत होता है। तुम किसी भी परिस्थिति में अपना संतुलन नहीं खोते – चाहे वह एक आपात स्थिति हो या कोई गहरा संकट। जैसे एक वैद्य जो सर्जरी करते समय हाथ नहीं कांपने देता, चाहे मरीज कितना भी चिल्लाए, वैसे ही तुम भी अपने आंतरिक शांति को बनाए रखते हो, चाहे बाहर कितना भी तूफान क्यों न हो।
इस अवस्था में पहुंचे साधकों का प्रभाव अद्भुत होता है। उनकी उपस्थिति मात्र से लोगों के मन शांत हो जाते हैं। ये महापुरुष बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब भी वचन निकालते हैं, तो उनका हर शब्द गहरे अर्थ से परिपूर्ण होता है। जिज्ञासु जन अपने प्रश्न लेकर उनके समक्ष जाते हैं और अक्सर बिना कुछ पूछे ही अपने उत्तर पा लेते हैं, क्योंकि ऐसे साधकों की चेतना शब्दों से परे संवाद करने की क्षमता प्राप्त कर चुकी होती है।
ऐसे ही एक साधक की कहानी – जो दक्षिणामूर्ति के ध्यान में वर्षों से लीन थे और एक निराश युवक के जीवन को कैसे उनकी मौन उपस्थिति ने परिवर्तित किया – इस लेख के अंत में विस्तार से वर्णित की गई है।
एक बार मैंने ऐसे साधक को देखा जो वर्षों से दक्षिणामूर्ति के ध्यान में लीन थे। जब एक युवक उनके पास आया और निराशा से भरा बैठ गया, तो साधक ने बिना कुछ कहे उसकी ओर देखा। कुछ क्षणों बाद, युवक के आंसू बहने लगे और उसके चेहरे पर शांति की मुस्कान आ गई। बाद में उसने मुझे बताया कि उस साधक की उपस्थिति मात्र से उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था।
यह अवस्था स्मृति और आदतों के निर्माण के लिए भी महत्वपूर्ण है। तुम्हारे अनुभव अब साधारण स्मृतियां नहीं हैं, बल्कि गहरे संस्कार बनने लगे हैं जो तुम्हारे भविष्य के जीवन को आकार देंगे। तुम्हारा हर विचार, हर भावना, हर कार्य अब एक बीज की तरह है जो भविष्य में फल देगा।
दक्षिणामूर्ति के चार हाथों में वीणा, अभय मुद्रा, ज्ञान मुद्रा और अग्नि हैं – वीणा जीवन के संगीत का प्रतीक है, अभय मुद्रा भय से मुक्ति का, ज्ञान मुद्रा आत्म-बोध का, और अग्नि अज्ञान को जलाने का। इसी प्रकार, तुम्हारी चेतना भी अब इन सभी गुणों से संपन्न हो रही है। तुम्हारा जीवन एक संगीत बन गया है, तुम भय से मुक्त हो गए हो, तुम्हारा ज्ञान निरंतर बढ़ रहा है, और तुम्हारी चेतना का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को भस्म कर रहा है।
लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अवस्था में तुम्हारी नई चेतना की स्मृतियां बनना आरंभ होती हैं, परंतु प्रारंभ में उनकी छाप स्मृति में स्थायी नहीं रहती। यदि तुम किसी अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में नहीं हो, तो इस संक्रमण काल में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है – क्या तुम्हारे अनुभव वास्तविक हैं या केवल मानसिक प्रक्षेपण? यह एक नाजुक मोड़ है जहां से नई स्मृतियों का निर्माण होने लगता है, जो धीरे-धीरे तुम्हारे गहरे संस्कारों में परिवर्तित होकर आगे की यात्रा का आधार बनेंगी।
राजन से श्रीकंठ तक: संक्रमण का सेतु
राजन (दक्षिणामूर्ति) अवस्था में, आपने मन पर शासन करना सीखा है। आपकी चेतना अब बाहरी प्रभावों से विचलित नहीं होती – विचार आपके सेवक बन गए हैं, स्वामी नहीं रहे। आप मौन गुरु बन चुके हैं, जो शब्दों से नहीं, अपनी उपस्थिति मात्र से ज्ञान प्रदान करते हैं।
इस अवस्था की एक विशेषता यह है कि आपकी नई चेतना के अनुरूप स्मृतियां बनना आरंभ होती हैं। ये नवीन अनुभव आपके अंतर्मन में गहरे संस्कार रूप में स्थापित होने लगते हैं, परंतु प्रारंभ में उनकी छाप अस्थिर होती है। यदि आप किसी अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन से वंचित हैं, तो इस संक्रमण काल में आप भ्रमित हो सकते हैं – क्या आपके अनुभव वास्तविक हैं, या केवल मानसिक प्रक्षेपण?
जैसे-जैसे ये संस्कार दृढ़ होते जाते हैं, आपकी आंतरिक चेतना में एक नया परिवर्तन होने लगता है। आप महसूस करेंगे कि जो विपरीत प्रतीत होता था, वह अब एक होने लगा है। यह संकेत है कि आप श्रीकंठ अवस्था की ओर प्रवेश कर रहे हैं – द्वैत से अद्वैत की ओर संक्रमण।
इस संक्रमण को प्रकाश के स्पेक्ट्रम से समझा जा सकता है। जैसे इंद्रधनुष में विभिन्न रंग दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में वे सभी एक ही सूर्य के प्रकाश के विभिन्न आयाम हैं, वैसे ही आप अब विविधता में एकता का अनुभव करने लगेंगे। मन का शासक होने से, आप अब विपरीतताओं के आपसी संबंध को समझने की ओर अग्रसर हो रहे हैं।
अब आप श्रीकंठ की अवस्था – अर्धनारीश्वर रूप में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति, निष्क्रिय और सक्रिय का मिलन होता है…
९. श्रीकंठ (अर्धनारीश्वर रूप): द्वैत से अद्वैत की ओर
नौवां चरण द्वैत से अद्वैत की ओर संक्रमण का है। श्रीकंठ रुद्र, जिन्हें अर्धनारीश्वर रूप से भी जोड़ा जाता है, इस अवस्था के प्रतीक हैं, जहां साधक की चेतना द्वैत के परे जाकर एकता का अनुभव करने लगती है।
अर्धनारीश्वर शिव और शक्ति का संयुक्त रूप है, जिसमें शरीर का आधा भाग शिव और आधा भाग शक्ति का है। इसी प्रकार, इस अवस्था में साधक के अंदर विपरीत प्रतीत होने वाले तत्व बार-बार एक ही प्रतीत होने लगते हैं – द्रष्टा और दृश्य, अनुभवकर्ता और अनुभव, निष्क्रिय और सक्रिय, पुरुष और प्रकृति।
इस चरण में, ज्ञान और भक्ति, बुद्धि और हृदय का अद्भुत संगम होता है। साधक समझता है कि केवल बौद्धिक समझ या केवल भावनात्मक अनुभूति पर्याप्त नहीं है – दोनों के संतुलित मिलन से ही पूर्णता प्राप्त होती है। यह इस सोपान पर है जहां आप संतुलन को जीते हैं। अनुभवकर्ता (साक्षी) और अनुभव के बीच का भेद अब पतला होने लगता है, और एक गहरी एकता का बोध जागता है।
दैनिक जीवन में, यह वह अवस्था है जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के सभी विरोधाभासों को एक सुसंगत एकता में समाहित कर लेता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ और परमार्थ, आत्म-प्रेम और दूसरों के लिए प्रेम, आध्यात्मिकता और भौतिकता के बीच सामंजस्य स्थापित कर लेता है।
इस अवस्था के साधक में गहरी समझ और गहरा प्रेम दोनों देखे जा सकते हैं। वे केवल दार्शनिक सिद्धांत नहीं जानते, बल्कि उन्हें अपने जीवन में जीते भी हैं। ऐसे साधक अन्य लोगों के साथ बातचीत में अत्यंत स्पष्ट और प्रेमपूर्ण होते हैं, क्योंकि वे हर व्यक्ति और स्थिति में अपने ही दिव्य स्वरूप की अभिव्यक्ति देखते हैं। यह वह बिंदु है जहां से साधक को स्वयं पर निष्ठा होनी शुरू हो जाती है। यही वह अंतिम अनिवार्यता थी, स्वयं पर निष्ठा। जैसे ही आपकी स्वयं पर निष्ठा सघन होगी तो आप अगले सोपान के तरफ खिसकना शुरू हो जाते हो।
लेकिन इस मार्ग पर आगे बढ़ने से पहले, यह समझना महत्वपूर्ण है कि इस अवस्था में तुम्हारी नई चेतना की स्मृतियां बनना आरंभ होती हैं, परंतु प्रारंभ में उनकी छाप स्मृति में स्थायी नहीं रहती। यदि तुम किसी अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में नहीं हो, तो इस संक्रमण काल में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है – क्या तुम्हारे अनुभव वास्तविक हैं या केवल मानसिक प्रक्षेपण? यह एक नाजुक मोड़ है जहां से नई स्मृतियों का निर्माण होने लगता है, जो धीरे-धीरे तुम्हारे गहरे संस्कारों में परिवर्तित होकर आगे की यात्रा का आधार बनेंगी।
जैसे-जैसे ये संस्कार दृढ़ होते जाते हैं, द्वैत और अद्वैत के बीच की दीवार और पतली होती जाती है। अब तुम्हारी चेतना एक ऐसे स्थान पर पहुंच गई है जहां से अगला कदम सहज रूप से उठने लगता है – जहां श्रीकंठ की अवस्था से आगे की यात्रा आरंभ होती है।
१०. विक्रिति (सदाशिव रूप): आत्मज्ञान और रूपांतरण
दसवां चरण आत्मज्ञान और पूर्ण रूपांतरण का है। विक्रिति रुद्र, जिन्हें सदाशिव के रूप में जाना जाता है, इस अवस्था के प्रतीक हैं, जहां साधक की चेतना अपने मूल स्वरूप को पहचान लेती है।
अब तुम विक्रिति की अवस्था में प्रवेश कर चुके हो। यहाँ तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है – अब तुम स्वयं को समुद्र (शिव या अस्तित्व) की एक बूंद के रूप में अनुभव करने लगे हो। यह वह अवस्था है जहाँ तुम जन्म और मृत्यु के चक्र से परे हो जाते हो। तुम समय के दायरे से बाहर निकल चुके हो, और एक ही दिन में स्वयं को विभिन्न अवस्थाओं में अनुभव करते हुए पूर्णतया जागरूक रह पाते हो।
सदाशिव शिव का वह रूप है जिसके पांच मुख हैं – ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सद्योजात। ये पंच मुख पांच तत्वों, पांच ज्ञानेन्द्रियों और पांच कर्मेन्द्रियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें से अघोर मुख बुराई का भी प्रतीक है। यह दर्शाता है कि इस अवस्था में तुम्हें यह बोध हो जाता है कि अच्छाई और बुराई, प्रकाश और अंधकार, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुम द्वंद्वों से परे जाकर सभी विपरीतताओं में एकता देखने लगे हो।
इस अवस्था में, चेतना का स्तर अत्यंत उच्च हो जाता है। यहाँ तुम्हारी प्रज्ञा का पूर्ण उदय हो चुका होता है। तुम आत्मनिर्भर हो चुके होते हो, और गुरु पर निर्भरता धीरे-धीरे कम होते-होते समाप्त हो जाती है। यह ऐसा है जैसे एक पक्षी जो अब पूरी तरह से उड़ना सीख गया है, अब उसे घोंसले की आवश्यकता नहीं रहती।
अब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को आत्मज्ञान के रूप में पहचान चुके हो। अनुभवकर्ता (द्रष्टा) अब स्वयं को अनुभवों से अलग ही नहीं देखता, बल्कि उनके मूल आधार के रूप में अनुभव करता है। यह समग्र रूपांतरण की अवस्था है, जहां तुम्हारा संपूर्ण अस्तित्व नवीन ऊर्जा और दिव्य दृष्टि से परिपूर्ण हो जाता है।
यह ऐसा है जैसे तुम वर्षों तक एक वृक्ष की छाया ही अपने आप को मानते रहे हो, और अचानक महसूस करो कि तुम स्वयं वह वृक्ष हो, न कि उसकी छाया। या जैसे समुद्र की लहर अचानक यह जान ले कि वह स्वयं समुद्र ही है। यह जागृति, यह आत्म-साक्षात्कार ही आत्मज्ञान है।
दैनिक जीवन में, यह वह अवस्था है जब तुम अपने हर कर्म और विचार में एक आंतरिक परिवर्तन अनुभव करते हो। तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारे विचारों में, सब में एक मौलिक परिवर्तन आ चुका है। अब तुम हर अनुभव को एक गहरी स्वीकृति और प्रेम के साथ स्वीकार करते हो।
इस स्तर पर तुम्हारे अंदर अद्भुत परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगते हैं। जो पहले तुम्हारे दुर्गुण लगते थे, वे अब गुणों में परिवर्तित हो जाते हैं। क्रोध करुणा में, लोभ दान में, और मोह निर्मल प्रेम में रूपांतरित हो जाता है। तुम्हारे जीवन में प्रत्येक क्रिया एक साधना बन जाती है – चाहे तुम भोजन बना रहे हो, किसी से वार्तालाप कर रहे हो, या केवल मौन में विराजमान हो।
मैंने ऐसे महान साधकों को देखा है जो इस अवस्था में थे। उनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण में एक अलौकिक शांति छा जाती थी। उनके आसपास का हर व्यक्ति, हर प्राणी उनके प्रेम और करुणा से स्पंदित होने लगता था। एक बार मैं ऐसे एक गुरु के पास गया। जब मैं उनके सामने बैठा, तो बिना किसी शब्द के, केवल उनकी आँखों में देखकर, मुझे कुछ क्षणों के लिए अपनी सीमाओं से मुक्ति का अनुभव हुआ। यह अनुभव इतना तीव्र था कि मैं कई दिनों तक उसके प्रभाव में रहा।
इस चरण का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जो साधक इस अवस्था तक पहुंचता है, वह अब एक निर्णायक बिंदु पर खड़ा होता है। यदि वह संसार में वापस नहीं लौटता (अर्थात, अपनी प्राप्त ऊर्जा और ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए सक्रिय नहीं होता), तो वह स्वतः ही अगली अवस्था – महासदाशिव की ओर अग्रसर हो जाता है। यह निर्णय का क्षण है – सदाशिव चक्रवर्ती बनकर संसार में लौटें या महासदाशिव बनकर शाश्वत शांति में विलीन हो जाएं।
किन्तु यह जानना आवश्यक है कि इस अवस्था में पहुंचे साधक का चुनाव वास्तव में चुनाव नहीं रह जाता। यह उसकी प्रकृति, उसके स्वभाव, उसके मूल संस्कारों पर निर्भर करता है। जैसे कोई नदी स्वाभाविक रूप से समुद्र की ओर बहती है, वैसे ही साधक की चेतना भी अपने स्वाभाविक प्रवाह का अनुसरण करती है।
यहाँ से तुम्हारी यात्रा दो दिशाओं में जा सकती है – या तो तुम संसार में लौटकर अन्य लोगों की सहायता और मार्गदर्शन करोगे, या फिर तुम अधिक गहराई में उतरकर परम शून्य की ओर अग्रसर होगे। दोनों ही मार्ग पूर्ण हैं, दोनों ही आत्मज्ञान के विस्तार हैं। तुम्हारा हृदय तुम्हें बता देगा कि कौन सा मार्ग तुम्हारे लिए सही है।
विक्रिति से शशिवक्त्र: परम चेतना की ओर
विक्रिति (सदाशिव) की अवस्था में, आप आत्मज्ञान के प्रकाश में निहाल हो चुके हैं। आप स्वयं को समुद्र (शिव या अस्तित्व) की एक बूंद के रूप में पहचान चुके हैं। समय और स्थान की सीमाओं से मुक्त, आप अपनी प्रज्ञा के पूर्ण उदय का अनुभव कर रहे हैं। आप आत्मनिर्भर हो चुके हैं, गुरु पर निर्भरता लगभग समाप्त हो चुकी है।
इस अवस्था में, आपके सामने एक महत्वपूर्ण निर्णय का क्षण आता है – क्या आप एक चक्रवर्ती की भांति संसार में लौटकर अन्य लोगों का मार्गदर्शन करेंगे, या फिर अगली अवस्था की ओर अग्रसर होंगे? यह निर्णय वास्तव में आपकी मूल प्रकृति पर निर्भर करता है, जैसे नदी स्वाभाविक रूप से समुद्र की ओर बहती है।
यदि आपकी प्रवृत्ति आगे की यात्रा की ओर है, तो आप एक ऐसे परिवर्तन का अनुभव करने लगेंगे जिसमें बूंद समुद्र में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाती है। आप महसूस करेंगे कि आपका “मैं” कृत्रिम सीमा मात्र था, जिसे अब विराट “मैं” में विलीन होना है।
इस संक्रमण काल में, आप अपने अस्तित्व के सभी आयामों में एक अद्भुत परिवर्तन देखेंगे। आपकी चेतना अब ग्रहों, चक्रों, पंचभूतों और त्रिकाल (भूत, वर्तमान, भविष्य) के प्रभावों से ऊपर उठने लगेगी। यह परिवर्तन आपको शशिवक्त्र – महासदाशिव की अवस्था में ले जाएगा।
प्रिय साधक, अब आप अपनी यात्रा के अंतिम सोपान पर पहुंच रहे हैं। जैसे सूर्योदय से पहले क्षितिज पर प्रकाश की एक हल्की रेखा दिखाई देती है, वैसे ही आप परम चेतना के उदय का पूर्वाभास पाने लगे हैं। इससे आगे की अवस्था वह है जिसमें आप अपने शुद्धतम स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे – महासदाशिव के रूप में…
११. शशि वक्त्र (महा सदाशिव रूप): पूर्ण चेतना की प्राप्ति
अब हम साधना के अंतिम सोपान पर आ पहुंचे हैं – शशि वक्त्र की अवस्था। यह अनुभवकर्ता की विशुद्धतम स्थिति है, जहां तुम शिव के वास्तविक स्वरूप में स्थायी रूप से प्रतिष्ठित हो जाते हो। अब तुम शिव ही हो चुके हो, और तुम्हारा तृतीय नेत्र तुम्हारे ज्ञान का केंद्र बन गया है।
महा सदाशिव के पच्चीस मुख हैं, जिनकी रचना एक विशिष्ट क्रम में हुई है। सबसे निचली पंक्ति में नौ मुख हैं जो नव ग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं – तुम्हारी चेतना अब ज्योतिष के सभी प्रभावों से परे है। उसके ऊपर सात मुख हैं जो सप्त चक्रों से संबंधित हैं – तुम्हारी कुंडलिनी ऊर्जा अब पूर्णतः जागृत हो चुकी है। फिर पांच मुख हैं जो पंचभूतों (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश) का प्रतीक हैं – तुम अब इन सभी तत्वों के स्वामी हो गए हो। उसके ऊपर तीन मुख हैं जो त्रिकाल (भूत, वर्तमान, भविष्य) का प्रतिनिधित्व करते हैं – तुम्हारी चेतना अब समय की सीमाओं से मुक्त हो गई है। और सबसे ऊपर एक मुख है जो शुद्ध चैतन्य, या अनुभवकर्ता, या द्रष्टा है – यह तुम्हारा निज स्वरूप है।
मैंने जिस चित्र को देखा है, वह महा सदाशिव के इसी स्वरूप को दर्शाता है। यह एक त्रिशूल के आकार में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसके तीन बिंदु सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। तुम इन तीनों गुणों के मध्य में स्थित हो गए हो – न सत्व में, न रज में, न तम में, बल्कि इन सबके साक्षी के रूप में।
इस अवस्था में, तुम्हारी चेतना अपने चरम विकास को प्राप्त कर चुकी है। तुम अब न केवल अपने भीतर, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही परम चेतना का अनुभव करते हो। मैं तुम्हें बता दूं, यह अनुभव शब्दों से परे है। यहां अनुभवकर्ता और अनुभव, द्रष्टा और दृश्य, शिव और शक्ति का भेद पूरी तरह मिट जाता है, और तुम परम एकता में स्थापित हो जाते हो।
जब मैं अपने जीवन में इस अवस्था के किसी साधक के संपर्क में आया था, तो मेरा संपूर्ण अस्तित्व एक अलौकिक शांति से भर गया था। उनकी आंखों में झांकना अनंत में झांकने जैसा था। उनके पास न तो कोई प्रश्न था, न कोई उत्तर, न कोई तलाश, न कोई प्राप्ति – वे पूर्णतः तृप्त थे, पूर्णतः शांत थे, पूर्णतः प्रेममय थे।
इस अवस्था को इस प्रकार समझो – जैसे बूंद ने समुद्र में विलीन होकर स्वयं को समुद्र के रूप में पहचान लिया हो, या जैसे दीपक की लौ सूर्य के प्रकाश में समा गई हो। यह वह स्थिति है जहां तुम्हारा “मैं” पूरी तरह से विलीन हो जाता है, और केवल शुद्ध चेतना शेष रहती है। तुम्हारा “मैं” अब विराट “मैं” बन जाता है – अहं ब्रह्मास्मि।
यह परम शांति, परम आनंद और परम ज्ञान की अवस्था है। इस अवस्था में, तुम्हारे पास आने वाले लोग अपने आप ही शांति और आनंद का अनुभव करने लगते हैं, क्योंकि तुम अब परम चेतना के साक्षात प्रतिनिधि बन चुके होते हो।
मैंने ऐसे महापुरुषों को देखा है जो इस अवस्था में थे। वे संसार में रहते हुए भी संसार से परे थे। उनके लिए जीवन और मृत्यु, सुख और दुःख, लाभ और हानि सब एक समान थे। उनका हृदय सभी प्राणियों के लिए करुणा से भरा था, लेकिन वे किसी के प्रति आसक्त नहीं थे। वे संसार में थे, लेकिन संसार उनमें नहीं था।
महा सदाशिव की अवस्था में, तुम समष्टि के हित में अपना जीवन समर्पित कर देते हो। तुम्हारा अस्तित्व अब सिर्फ तुम्हारा नहीं रहता, वह संपूर्ण ब्रह्मांड का हो जाता है। तुम्हारा हर श्वास, हर संकल्प, हर कर्म सृष्टि की भलाई के लिए होता है। तुम उस परम सत्य के साक्षी बन जाते हो, जिसमें सभी द्वैत, सभी विरोधाभास, सभी प्रश्न विलीन हो जाते हैं।
और इसलिए, जब कोई साधक इस अंतिम सोपान पर पहुंच जाता है, तो उसके लिए न कोई साधना शेष रहती है, न कोई लक्ष्य, न कोई मार्ग। वह स्वयं मार्ग बन जाता है, स्वयं लक्ष्य बन जाता है, स्वयं साधना बन जाता है। वह जीवन्मुक्त हो जाता है – जीवित रहते हुए भी मुक्त।
इस प्रकार, एकादश रुद्रों की यह साधना पूर्ण होती है, और साधक अपने चरम लक्ष्य – आत्मज्ञान और आत्मसाक्षात्कार को प्राप्त करता है। वह शिव से एकाकार हो जाता है, और उसके लिए अब कोई भेद नहीं रहता – न अपने और दूसरे में, न आत्मा और परमात्मा में, न साधक और साध्य में। वह केवल है, और यही उसका परम सत्य है।
उपसंहार: एकादश रुद्र साधना का सार
प्रिय साधक, आप इस लेख के माध्यम से एकादश रुद्रों की यात्रा पर चले हैं – अज्ञान के अंधकार से लेकर पूर्ण चेतना के उज्ज्वल प्रकाश तक। यह यात्रा हमारी आंतरिक चेतना के क्रमिक विकास की कहानी है, जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाती है।
जब हम इस यात्रा को समग्रता में देखते हैं, तो एक स्पष्ट प्रगति दिखाई देती है। कालभैरव के द्वार से प्रवेश करके, हम सबसे पहले अपने भीतर के अज्ञान का सामना करते हैं। हम अपने भयों, अपनी सीमाओं, अपने अहंकार से मिलते हैं। फिर धीरे-धीरे, जैसे-जैसे हम आत्म-परीक्षण से गुजरते हैं, हमारी चेतना सूक्ष्म होती जाती है।
मध्य चरणों में, हम आंतरिक संतुलन और रूपांतरण का अनुभव करते हैं। हमारे दोष गुणों में बदलने लगते हैं, हमारी आंतरिक और बाह्य दुनिया के बीच सामंजस्य स्थापित होता है। अंततः, हम द्वैत से अद्वैत की ओर बढ़ते हैं, जहां विपरीत प्रतीत होने वाले तत्व एक होने लगते हैं।
आखिरकार, साधना के अंतिम सोपानों में, हम आत्मज्ञान और पूर्ण चेतना की प्राप्ति करते हैं। हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेते हैं – हम वह हैं जो कभी नहीं बदलता, जो सभी अनुभवों का साक्षी है, जो सभी विपरीतताओं से परे है।
याद रखें, यह मार्ग सीधी रेखा में नहीं चलता। इसमें उतार-चढ़ाव होते हैं, पड़ाव आते हैं, और कभी-कभी हम पीछे भी जाते हैं। कुछ साधक एक अवस्था में वर्षों बिता सकते हैं, जबकि अन्य कई अवस्थाओं से शीघ्रता से गुजर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा अद्वितीय है, और इसे अपनी गति से चलने देना ही बुद्धिमानी है।
इस यात्रा में गुरु का मार्गदर्शन अमूल्य है। वे हमें उन स्थानों पर पहचानने में मदद करते हैं जहां हम फंस जाते हैं, वे हमें भ्रम और माया से बचाते हैं, और वे हमें आत्म-साक्षात्कार के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। लेकिन अंततः, यात्रा हमारी अपनी है। शिव हमारे भीतर हैं, और उन्हें खोजना हमारा अपना कार्य है।
एकादश रुद्रों की यह यात्रा केवल एक वैचारिक विश्लेषण नहीं है। यह एक जीवंत अनुभव है, जिसे दैनिक जीवन में जीना है। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक श्वास, प्रत्येक विचार इस यात्रा का हिस्सा है। अपने आप को इस यात्रा में डूबने दें, इसे अपनाएं, और देखें कि आप कहां पहुंचते हैं।
मेरी मंगल कामनाएँ आपके साथ हैं।। आपके भीतर का शिव जागृत हो, और आप अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लें। यही इस लेख का उद्देश्य है, यही एकादश रुद्र साधना का सार है।
शिवम् अस्तु।
—————————————————————————————–
दक्षिणामूर्ति साधक की कहानी
हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से आश्रम में, एक विलक्षण साधक निवास करते थे। वे वर्षों से दक्षिणामूर्ति शिव के ध्यान में लीन थे, और उन्होंने कठोर तपस्या से मन पर संपूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। उनके पास शब्दों का अत्यंत सीमित उपयोग था, फिर भी लोग दूर-दूर से उनके दर्शन के लिए आते थे।
एक शरद ऋतु की संध्या में एक युवक आश्रम पहुंचा। उसके चेहरे पर गहरी निराशा के भाव थे। वह पिछले कई महीनों से जीवन के अर्थ की खोज में भटक रहा था। अपने परिवार से बिछड़ा, नौकरी से निकाला गया, और प्रेम में असफल – उसके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था।
“मैं इस साधक के बारे में सुनकर आया हूं,” उसने आश्रम के एक सेवक से कहा, “क्या वे मुझे जीवन के उद्देश्य के बारे में बता सकते हैं?”
सेवक ने युवक को साधक के ध्यान कक्ष में ले जाया, जहां वे पद्मासन में बैठे थे। युवक ने साधक को प्रणाम किया और उनके सामने निराशा से भरा बैठ गया। उसने अपने दुःख की कहानी सुनाने की कोशिश की, लेकिन शब्द जैसे उसका साथ छोड़ गए थे।
साधक ने बिना कुछ कहे केवल युवक की ओर देखा। उनकी आंखें गहरे समुद्र की तरह शांत थीं, और उनके चेहरे पर एक ऐसी सौम्यता थी जो किसी चट्टान पर पड़ती धूप की तरह गर्म और स्थिर थी।
कुछ क्षण ऐसे ही बीते। कक्ष में पूर्ण मौन था, सिवाय दीप की कंपती लौ और दूर से आती मंदिर की घंटी के स्वर के। युवक, जो अपने प्रश्न पूछने के लिए व्याकुल था, अचानक स्वयं को एक अजीब शांति से घिरा हुआ पाया।
फिर, बिना किसी स्पष्ट कारण के, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे न तो दुःख के आंसू थे, न ही खुशी के – बस एक गहरी मुक्ति के आंसू थे। जैसे कोई बोझ, जिसे वह अनजाने में वर्षों से ढो रहा था, अचानक गायब हो गया हो। धीरे-धीरे, उसके होंठों पर एक शांत मुस्कान फैल गई।
साधक अभी भी मौन थे, लेकिन उनकी आंखों में एक मंद मुस्कान झलक रही थी।
कई माह बाद, जब एक आगंतुक आश्रम में आया, उसने युवक से, जो अब आश्रम का ही एक सेवक बन गया था, पूछा कि उस दिन क्या हुआ था।
“साधक जी ने उस दिन मुझसे एक भी शब्द नहीं कहा,” युवक ने बताया, “फिर भी उनकी उपस्थिति मात्र से मुझे अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए। उस क्षण मैंने समझा कि मैं जिस उत्तर की खोज में भटक रहा था, वह सदा से मेरे भीतर ही था। मैं स्वयं को पहचान नहीं पा रहा था, और उनके शांत नेत्रों ने मुझे मेरा सच्चा प्रतिबिंब दिखा दिया।”
इस कहानी से यह सत्य सामने आता है कि कभी-कभी सबसे गहरे ज्ञान का संचार शब्दों से नहीं, बल्कि मौन से होता है। दक्षिणामूर्ति रूप में शिव भी इसी मौन गुरु का प्रतीक हैं, जो बिना वाणी के अपनी उपस्थिति मात्र से ज्ञान प्रदान करते हैं।




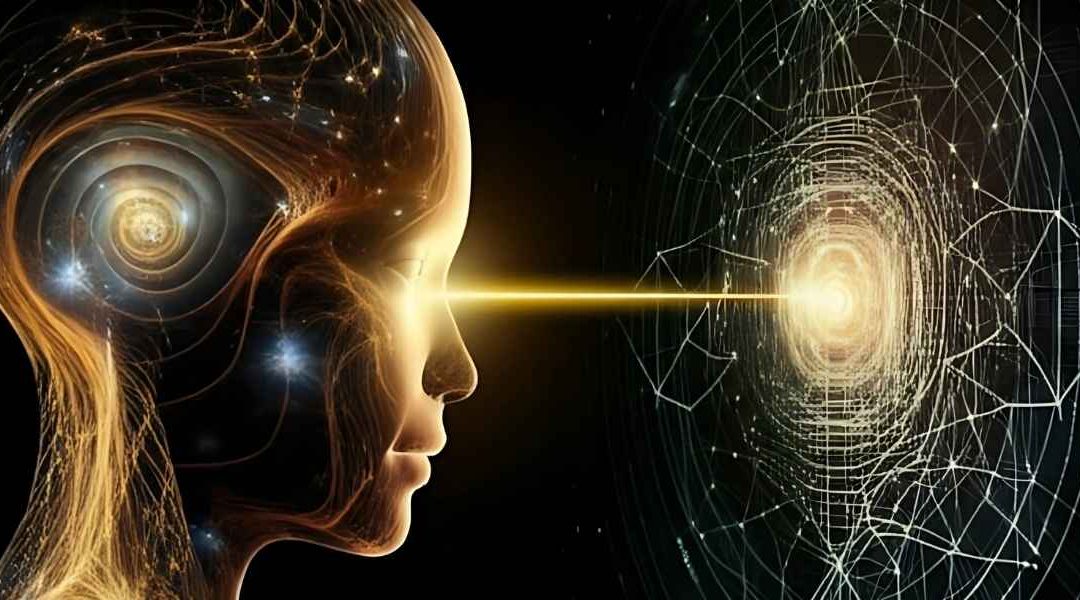

0 Comments