हम सभी अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं। बाहरी दुनिया में हम पढ़ाई, नौकरी और व्यापार से आगे बढ़ते हैं, लेकिन आंतरिक उन्नति के लिए हमें अपनी वृत्तियों (स्वभाव और आदतों) को समझना होगा। ज्ञान मार्ग पर चलने का अर्थ है – देखना, समझना और जागरूक रहना। इस लेख में हम छः क्षेत्रों में धार्मिक (आध्यात्मिक विकास में सहायक) और अधार्मिक (आध्यात्मिक विकास में बाधक) वृत्तियों को सरल उदाहरणों के साथ समझेंगे।
याद रखें, हम इन वृत्तियों के “देखने वाले” या “साक्षी” हैं। जैसे सिनेमा हॉल में बैठकर हम फिल्म देखते हैं, वैसे ही हम अपने जीवन की इन वृत्तियों को देखते और अनुभव करते हैं। हम इन्हें देखने वाले हैं, जिसे अनुभवकर्ता, दृष्टा, साक्षी या चैतन्य भी कहते हैं।
1. व्यवहार (Behavior) – हम कैसे कार्य करते हैं
धार्मिक वृत्तियाँ (सहायक आदतें):
उदाहरण 1: साधना में तल्लीनता राजेश एक बैंक मैनेजर हैं। हर दिन सुबह 5 बजे उठकर वह एक घंटा ध्यान करते हैं। कार्यालय में भी वह थोड़ी-थोड़ी देर अपनी श्वास पर ध्यान देते रहते हैं। उनका बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, बेटी डॉक्टर बनना चाहती है। राजेश अपने परिवार की आवश्यकताएँ पूरी करते हैं, लेकिन उनका मन हमेशा आध्यात्मिक उन्नति पर केंद्रित रहता है। वह अपने परिवार से कहते हैं, “मेरा लक्ष्य आत्म-साक्षात्कार है, बाकी सब उसके लिए साधन मात्र हैं।”
उदाहरण 2: विवेकपूर्ण एकांत सुमन एक स्कूल शिक्षिका हैं। वह अपना काम पूरी लगन से करती हैं, लेकिन सोशल मीडिया और पार्टियों से दूर रहती हैं। उनकी सहेली प्रीति पूछती है, “तुम इन सबसे दूर क्यों रहती हो? क्या हम लोगों से नफरत करती हो?” सुमन मुस्कुराकर कहती हैं, “बिलकुल नहीं। मैं सभी को प्यार करती हूँ, लेकिन शोर-शराबे से मेरा मन विचलित होता है। एकांत में मुझे अपने भीतर का संगीत सुनाई देता है।”
उदाहरण 3: सरलता और न्यूनतावादी जीवन अमित एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। वह अच्छी कमाई करते हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ तीन जोड़ी कपड़े हैं, एक साधारण मोबाइल फोन और कोई वाहन नहीं। एक दिन उनके मित्र ने पूछा, “तुम इतना कमाते हो फिर भी इतनी सादगी से क्यों रहते हो?” अमित ने मुस्कुराकर कहा, “जितनी कम चीजें, उतनी कम चिंताएँ। मेरा मन हमेशा शांत और प्रसन्न रहता है।”
अधार्मिक वृत्तियाँ (बाधक आदतें):
उदाहरण 1: सांसारिक आसक्ति विनोद हर महीने नया स्मार्टफोन, नए कपड़े और नए गैजेट्स खरीदते हैं। वह अपनी नई खरीदारी के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हैं। एक दिन उनके गुरु ने उन्हें बताया, “तुम ध्यान में गहरे नहीं जा पा रहे हो क्योंकि तुम्हारा मन हमेशा नई चीजों की चिंता में उलझा रहता है।” विनोद इस बात को समझ तो गए, लेकिन आदत बदल नहीं पाए।
उदाहरण 2: पक्षपात और विषमता मीना एक बड़े कार्यालय में मैनेजर हैं। वह अपने पसंदीदा कर्मचारियों को आसान काम और अतिरिक्त छुट्टियाँ देती हैं, जबकि अन्य कर्मचारियों से कठोर व्यवहार करती हैं। मीना साथ ही आध्यात्मिक संगोष्ठियों में भी जाती हैं, लेकिन जब एक साधु ने उन्हें बताया कि “सबके प्रति समान व्यवहार ही आध्यात्मिकता की नींव है,” तब भी उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया।
उदाहरण 3: अहंकार-प्रेरित व्यवहार सुरेश 10 सालों से योग और ध्यान कर रहे हैं। जब भी कोई उनसे मिलता है, वह कहते हैं, “मैं रोज 2 घंटे ध्यान करता हूँ, तुम कितना करते हो?” वह हर बातचीत में अपनी आध्यात्मिक प्रगति और अनुभवों का उल्लेख करते हैं। उनके एक मित्र ने टिप्पणी की, “सुरेश को अपनी साधना का इतना अहंकार है कि वह वास्तविक आध्यात्मिकता से दूर होते जा रहे हैं।”
2. वाणी (Speech) – हम कैसे बोलते हैं
धार्मिक वृत्तियाँ:
उदाहरण 1: मधुर और शांत वाणी करण एक बिजनेस मीटिंग में थे। एक सहकर्मी ने गलत आंकड़े प्रस्तुत किए और सभी उस पर चिल्लाने लगे। करण ने शांति से उठकर धीमी और मधुर आवाज में कहा, “शायद हम पहले आंकड़ों को दोबारा जांच लें, फिर निर्णय लें।” उनकी शांत वाणी ने पूरे माहौल को शांत कर दिया।
उदाहरण 2: सत्य का अभ्यास रीना के बेटे ने स्कूल में शरारत की थी। जब प्रिंसिपल ने पूछा, रीना कह सकती थीं, “मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता,” लेकिन उन्होंने सच बोला: “हाँ, वह गलती कर सकता है। मैं उससे बात करूँगी और सुनिश्चित करूँगी कि यह दोबारा न हो।” घर आकर उनके बेटे ने पूछा, “आपने मेरा बचाव क्यों नहीं किया?” रीना ने समझाया, “सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है, बेटा। झूठ से हम अपने आप को धोखा देते हैं।”
उदाहरण 3: मौन का महत्व अनिल एक आईटी कंपनी में काम करते हैं। ऑफिस में सभी लोग लंच के समय गपशप करते और दूसरों की बुराई करते हैं। अनिल शांति से अपना खाना खाते हैं और केवल जरूरी बातें ही करते हैं। एक दिन एक सहकर्मी ने पूछा, “तुम इतने चुप क्यों रहते हो?” अनिल ने मुस्कुराकर कहा, “जो समय बातों में जाता है, वह मेरे अंदर की आवाज सुनने में जा सकता है।”
अधार्मिक वृत्तियाँ:
उदाहरण 1: अनावश्यक वार्तालाप सविता हर किसी की बात काटती हैं और बिना रुके बोलती रहती हैं। एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सत्संग में भी, गुरुजी के बोलने के बीच वह अपनी बात रखने लगीं। बाद में उनकी मित्र ने कहा, “तुम्हें पता भी है कि आज गुरुजी ने क्या महत्वपूर्ण ज्ञान दिया?” सविता उत्तर नहीं दे पाईं क्योंकि वह अपनी बातों में इतनी उलझी थीं कि सुन ही नहीं पाईं।
उदाहरण 2: कठोर वाणी राहुल एक अच्छे ध्यानी हैं, लेकिन जब कोई छोटी गलती होती है, तो वह अपने परिवार पर चिल्लाते हैं। एक दिन उनकी पत्नी ने पूछा, “आप इतना ध्यान करते हैं, फिर भी इतना गुस्सा क्यों करते हैं?” राहुल को अहसास हुआ कि उनकी कठोर वाणी उनकी आध्यात्मिक प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है।
उदाहरण 3: निंदा और आलोचना मनोज और उनके दोस्त हर शाम चाय की दुकान पर मिलते हैं और अपने गुरु, साथी साधकों और अन्य लोगों की निंदा करते हैं। एक दिन एक बुजुर्ग साधु वहां से गुजरे और उन्होंने मनोज से पूछा, “बेटा, क्या तुम जानते हो, जब तुम किसी की निंदा करते हो, तो वह पाप तुम्हें और वह पुण्य उसे मिलता है?” मनोज को अपनी गलती का अहसास हुआ।
3. विचार (Thoughts) – हम कैसे सोचते हैं
धार्मिक वृत्तियाँ:
उदाहरण 1: चेतना में निवास अंजलि एक व्यस्त डॉक्टर हैं। मरीजों की भीड़, फोन कॉल, और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच, वह एक खास क्षमता विकसित कर चुकी हैं। वह हर स्थिति को देखती हैं, लेकिन उसमें खोती नहीं हैं। जैसे कोई आकाश से बादलों को देखता है, वैसे ही वह अपने विचारों को देखती रहती हैं। एक दिन उनकी सहकर्मी ने पूछा, “इतने तनाव में भी आप इतनी शांत कैसे रहती हैं?” अंजलि ने मुस्कुराकर कहा, “मैं विचारों की नहीं, विचारों को देखने वाली चेतना हूँ।”
उदाहरण 2: आवश्यकतानुसार विचार मोहन एक वकील हैं। कोर्ट में तर्क-वितर्क करते समय वह अपनी बुद्धि का पूरा उपयोग करते हैं। लेकिन काम खत्म होते ही, वह सभी विचारों को एक तरफ रख देते हैं – बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई कलम को मेज पर रख दे। घर पर, बगीचे में बैठकर, वह सिर्फ फूलों को देखते हैं, पक्षियों की आवाज सुनते हैं – बिना किसी विचार के। उनके मित्र ने पूछा, “तुम इतनी आसानी से विचारों को रोक कैसे लेते हो?” मोहन ने कहा, “मैं रोकता नहीं, बस देखता हूँ। जैसे आकाश बादलों को आने-जाने देता है, वैसे ही मैं विचारों को।”
उदाहरण 3: समभाव नीता के व्यापार में अचानक बड़ा नुकसान हुआ। उनके कुछ मित्र बहुत परेशान हुए, कुछ ने सलाह दी, कुछ ने आलोचना की। नीता शांत बैठी सब देख रही थीं। उनकी बेटी ने पूछा, “माँ, आप इतने बड़े नुकसान पर भी इतनी शांत कैसे हैं?” नीता ने कहा, “बेटा, जीवन लाभ और हानि दोनों से भरा है। अगर मैं लाभ पर खुश होती हूँ और हानि पर दुखी, तो मेरी शांति हमेशा दूसरों के हाथ में रहेगी। मैं सब स्थितियों में एक जैसी रहना चाहती हूँ।”
अधार्मिक वृत्तियाँ:
उदाहरण 1: विचारों में उलझाव रमेश हर रात बिस्तर पर लेटकर अगले दिन के काम, बच्चों की पढ़ाई, पैसों की समस्या, और पुराने विवादों के बारे में सोचते रहते हैं। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा। एक रात उनकी पत्नी ने देखा कि वह करवटें बदल रहे हैं। पूछने पर रमेश ने कहा, “मैं सोच रहा था कि 10 साल पहले अगर वह प्रमोशन मिला होता तो आज हमारी स्थिति कैसी होती।” उनकी पत्नी ने कहा, “10 साल पुरानी बात को सोचकर आज की नींद क्यों खराब कर रहे हो?”
उदाहरण 2: द्वैत में जीना सीमा हर चीज को “अच्छा-बुरा” के चश्मे से देखती हैं। एक दिन उनका बेटा स्कूल से आया और बताया कि उसे दूसरा स्थान मिला है। सीमा नाराज हो गईं, “पहला क्यों नहीं? तुमने पूरी मेहनत नहीं की!” जब गुरुजी के प्रवचन में गए, तो उन्होंने कहा, “आज का प्रवचन अच्छा था, कल वाला ज्यादा अच्छा था, परसों वाला बेकार था।” उनकी मित्र ने कहा, “सीमा, तुम हर चीज को अच्छा-बुरा में बांटकर खुद ही दुखी हो जाती हो।”
उदाहरण 3: अहं-केंद्रित सोच विवेक एक अच्छे योग शिक्षक हैं, लेकिन उनके विचारों में हमेशा “मैं” और “मेरा” होता है। “मेरी क्लास,” “मेरे छात्र,” “मेरी तकनीक,” “मेरी प्रसिद्धि।” एक बार उनके गुरु ने कहा, “विवेक, जब तक तुम्हारे विचारों में ‘मैं’ है, तब तक तुम सच्चे ‘स्व’ को नहीं जान पाओगे। ‘मैं’ का अर्थ है ‘अहंकार’ जो आत्मा का आवरण है।”
4. संबंध (Relationships) – हम दूसरों से कैसे जुड़ते हैं
धार्मिक वृत्तियाँ:
उदाहरण 1: आंतरिक वैराग्य प्रकाश एक सफल बिजनेसमैन हैं। उनका परिवार, व्यापार और सामाजिक दायित्व सब कुछ है, लेकिन अंदर से वे इन सबसे अनासक्त हैं। जब उनके बेटे ने पूछा, “पिताजी, आप हमसे प्यार नहीं करते?” प्रकाश ने प्यार से समझाया, “बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हर संभव तरीके से तुम्हारी देखभाल करता हूँ। लेकिन मेरा प्यार बंधन नहीं है। मैं तुम्हें अपनी संपत्ति नहीं मानता, तुम्हारी अपनी जिंदगी है। मैं वहां हूँ जब तुम्हें जरूरत हो, लेकिन मानसिक रूप से मैं स्वतंत्र हूँ, और तुम्हें भी स्वतंत्र रहने देता हूँ।”
उदाहरण 2: गुरु-शिष्य संबंध मीरा एक प्रोफेसर हैं। वह अपने गुरु को अपने जीवन का केंद्र मानती हैं। जब उनके मित्र ने पूछा, “तुम इतनी शिक्षित होकर भी अपने गुरु की हर बात क्यों मानती हो?” मीरा ने कहा, “मेरी शिक्षा ने मुझे इतना ही सिखाया है कि मैं जितना जानती हूँ, वह सागर में एक बूंद के समान है। मेरे गुरु मुझे उस अनंत सागर से जोड़ते हैं। मेरा उनसे सम्बंध ही मेरा सबसे कीमती संबंध है।”
उदाहरण 3: समदृष्टि अरुण एक बैंक के सुरक्षा गार्ड हैं। बैंक के मैनेजर से लेकर सफाई कर्मचारी तक, वह सभी से एक जैसा व्यवहार करते हैं। एक दिन जब बैंक के मालिक आए, तब भी अरुण ने उन्हें वैसे ही नमस्ते की जैसे वह हर रोज सबको करते हैं। मालिक ने इसे नोटिस किया और पूछा, “आप सबको एक जैसा सम्मान कैसे दे पाते हैं?” अरुण ने सहजता से कहा, “मेरे लिए सब एक जैसे हैं। सभी में वही चेतना है, केवल भूमिकाएँ अलग हैं।”
अधार्मिक वृत्तियाँ:
उदाहरण 1: सांसारिक आसक्ति रोहित अपने बेटे के प्रति इतने आसक्त हैं कि उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं, यहाँ तक कि गलत चीजें भी। एक दिन उनके बेटे ने कहा, “पापा, मुझे एक नई बाइक चाहिए, वरना मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा।” रोहित जानते थे कि उनका बेटा अभी बाइक चलाने के लिए बहुत कम उम्र का है, फिर भी उन्होंने बाइक खरीद दी। एक बुजुर्ग पड़ोसी ने कहा, “रोहित, यह प्यार नहीं, आसक्ति है। सच्चा प्यार वह है जो बच्चे के भविष्य के बारे में सोचता है, न कि वर्तमान की खुशी के लिए उसके भविष्य को खतरे में डालता है।”
उदाहरण 2: द्वेषपूर्ण पृथकता सुधीर एक छोटे शहर से बड़े शहर चले गए और धीरे-धीरे अपने परिवार और पुराने दोस्तों से संपर्क कम कर दिया। जब भी कोई उनसे मिलने की कोशिश करता, वह कहते, “मैं आध्यात्मिक हो गया हूँ, इन सांसारिक संबंधों से क्या लेना-देना।” उनकी माँ ने फोन पर कहा, “बेटा, आध्यात्मिकता का अर्थ लोगों से नफरत करना नहीं, सबसे प्रेम करना है। तुम्हारा अलगाव घृणा से प्रेरित है, वैराग्य से नहीं।”
उदाहरण 3: संबंधों की अनदेखी राधा एक आध्यात्मिक साधिका हैं। वह दिन भर आश्रम में रहती हैं और घर की जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करती हैं। उनके बच्चे और पति अपना खाना खुद बनाते हैं, कपड़े खुद धोते हैं। एक दिन उनके गुरु ने कहा, “राधा, तुम्हारा कर्तव्य भी तुम्हारी साधना का हिस्सा है। तुम आश्रम में घंटों बैठकर ध्यान करती हो, लेकिन अपने परिवार के प्रति कर्तव्यों की अनदेखी करती हो। यह सच्ची आध्यात्मिकता नहीं है।”
5. मनोरंजन (Recreation) – हम अपना खाली समय कैसे बिताते हैं
धार्मिक वृत्तियाँ:
उदाहरण 1: सत्संग में आनंद दीपक एक बिजी आईटी प्रोफेशनल हैं। हर शनिवार-रविवार वह अपने नजदीकी आश्रम में सत्संग में जाते हैं। उनके दोस्त उन्हें पार्टी और मॉल में बुलाते हैं, लेकिन दीपक कहते हैं, “मुझे सत्संग में जो शांति और आनंद मिलता है, वह कहीं और नहीं। दो घंटे के सत्संग के बाद मेरा मन पूरे हफ्ते के थकान से मुक्त हो जाता है।”
उदाहरण 2: स्व-रमण सुनीता एक बैंक में काम करती हैं। कार्यालय के बाद उनके सहकर्मी शॉपिंग, मूवी या रेस्तरां में जाते हैं, लेकिन सुनीता अपने कमरे में शांति से बैठना पसंद करती हैं। कभी पुस्तक पढ़ती हैं, कभी बस खिड़की से बाहर देखती हैं, कभी अपनी सांसों को महसूस करती हैं। एक दिन उनकी सहेली ने पूछा, “तुम्हें अकेले बोर नहीं होता?” सुनीता ने मुस्कुराकर कहा, “मैं कभी अकेली नहीं हूँ। मैं अपने आप के साथ हूँ, और यह मेरा सबसे अच्छा साथी है।”
उदाहरण 3: प्रकृति के साथ एकता रवि एक बिजनेसमैन हैं। हर महीने वह दो दिन के लिए पहाड़ों या जंगल में जाते हैं। वहां वह मोबाइल बंद कर देते हैं और सिर्फ प्रकृति के साथ समय बिताते हैं। एक बार उनके एक व्यापारिक साथी ने पूछा, “तुम वहां क्या करते हो?” रवि ने कहा, “वहां मैं कुछ नहीं करता, बस होता हूँ। पेड़ों को देखता हूँ, पक्षियों को सुनता हूँ, पहाड़ों को निहारता हूँ। प्रकृति में रहकर मुझे अपना असली स्वरूप याद आता है।”
उदाहरण 4: सेवा में आनंद गीता एक रिटायर्ड शिक्षिका हैं। वह हर रविवार स्लम एरिया के बच्चों को मुफ्त पढ़ाती हैं। जब उनकी बेटी ने पूछा, “माँ, आप इस उम्र में भी इतनी मेहनत क्यों करती हैं?” गीता ने कहा, “बेटा, यह मेहनत नहीं, मेरा आनंद है। जब मैं इन बच्चों की आँखों में ज्ञान की चमक देखती हूँ, तो मुझे ऐसी खुशी मिलती है जो पैसों से नहीं मिल सकती।”
अधार्मिक वृत्तियाँ:
उदाहरण 1: इंद्रिय-सुख में लिप्तता अजय हर शाम क्लब में जाते हैं, शराब पीते हैं, और देर रात तक पार्टी करते हैं। वह कहते हैं, “जीवन का मजा लेना चाहिए।” लेकिन हर सुबह वह सिरदर्द और थकान के साथ उठते हैं, और दिनभर चिड़चिड़े बने रहते हैं। एक दिन उनके एक मित्र, जो योग शिक्षक हैं, ने कहा, “अजय, इंद्रियों का सुख क्षणिक होता है और अंत में दुख ही देता है। असली सुख भीतर है, जो कभी कम नहीं होता।”
उदाहरण 2: आत्म-विस्मरण वाला मनोरंजन पूजा सोशल मीडिया पर हर दिन 5-6 घंटे बिताती हैं। वह दूसरों की पोस्ट देखती हैं, कमेंट करती हैं, और अपनी फोटो अपलोड करती हैं। एक दिन उनकी दादी ने पूछा, “बेटी, तुम इस छोटे से स्क्रीन में क्या देखती रहती हो?” पूजा ने कहा, “दादी, यह मेरी दुनिया है।” दादी ने समझाया, “बेटी, यह तुम्हारी दुनिया नहीं, माया है जो तुम्हें अपने असली स्वरूप को भुला रही है। जो समय इसमें जा रहा है, उसमें तुम अपने अंदर झांक सकती हो।”
उदाहरण 3: कर्तव्य-विमुखता विशाल रोज काम से आकर 4-5 घंटे वीडियो गेम खेलते हैं। इस बीच उनकी पत्नी घर का सारा काम अकेले करती है, बच्चे उनके ध्यान की मांग करते हैं, लेकिन वह गेम में इतने खोए रहते हैं कि कुछ सुनते ही नहीं। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, “तुम्हारा मनोरंजन तुम्हारे कर्तव्यों से अधिक महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है?” विशाल को अपनी गलती का अहसास हुआ।
6. स्वास्थ्य (Health) – हम अपने शरीर के प्रति कैसे हैं
धार्मिक वृत्तियाँ:
उदाहरण 1: साधन के रूप में शरीर राजेंद्र 60 वर्ष के हैं। वह हर सुबह 30 मिनट योग करते हैं, संतुलित भोजन करते हैं, और पर्याप्त नींद लेते हैं। जब उनके मित्र ने पूछा, “तुम इतने नियमित क्यों हो?” राजेंद्र ने कहा, “मेरा शरीर मेरी आत्मा का मंदिर है और साधना का साधन है। जैसे कार को अच्छी हालत में रखना जरूरी है यात्रा के लिए, वैसे ही शरीर को स्वस्थ रखना आवश्यक है आत्म-यात्रा के लिए।”
उदाहरण 2: मार्ग के प्रति समर्पण सरिता को डॉक्टर ने बताया कि उन्हें एक गंभीर बीमारी है। लेकिन वह इससे परेशान नहीं हुईं। उन्होंने अपना इलाज कराया, लेकिन साथ ही अपनी साधना भी जारी रखी। उनके बेटे ने पूछा, “माँ, आप इतनी शांत कैसे हैं?” सरिता ने कहा, “बेटा, मैं अपने मार्ग के प्रति समर्पित हूँ। यह शरीर अनित्य है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। मैं अपने शरीर का ध्यान रखती हूँ, लेकिन इसे ही सब कुछ नहीं मानती।”
उदाहरण 3: संतुलित स्वास्थ्य दृष्टिकोण अमन एक युवा डॉक्टर हैं। वह अपने रोगियों को न केवल दवाइयां देते हैं, बल्कि जीवनशैली में संतुलन के बारे में भी सलाह देते हैं। अपने एक रोगी से उन्होंने कहा, “शरीर, मन और आत्मा – इन तीनों का संतुलन स्वास्थ्य का असली मंत्र है। न तो शरीर की उपेक्षा करें और न ही इसे सर्वोपरि मानें। यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण, लेकिन अस्थायी, हिस्सा है।”
अधार्मिक वृत्तियाँ:
उदाहरण 1: शरीर के प्रति आसक्ति नेहा हर दिन 3-4 घंटे जिम में बिताती हैं, सौंदर्य उत्पादों पर हजारों रुपये खर्च करती हैं, और सोशल मीडिया पर अपनी फिटनेस की फोटो पोस्ट करती हैं। एक बार उनके गुरु ने कहा, “नेहा, तुम अपने शरीर की देखभाल करो, यह अच्छी बात है। लेकिन शरीर के प्रति यह आसक्ति तुम्हें आत्मा से दूर ले जा रही है। जो समय तुम आईने के सामने बिताती हो, उसका थोड़ा हिस्सा अपने भीतर झांकने में भी लगाओ।”
उदाहरण 2: सिद्धियों के मोह कमल नियमित रूप से कुछ विशेष ध्यान तकनीकें करते हैं। उन्हें कुछ विशेष अनुभव होने लगे हैं – कभी प्रकाश दिखता है, कभी आवाजें सुनाई देती हैं। वह इन अनुभवों के बारे में सबको बताते हैं और कहते हैं, “जैसे-जैसे मुझे अधिक शक्तियां मिलेंगी, मैं और तेजी से प्रगति करूंगा।” उनके गुरु ने एक दिन समझाया, “कमल, ये सिद्धियां रास्ते के पत्थर हैं, मंजिल नहीं। इनमें अटकना अपने लक्ष्य से भटकना है। सच्ची उन्नति इन शक्तियों में नहीं, इनसे पार जाने में है।”
उदाहरण 3: शरीर के प्रति अवहेलना संतोष एक कट्टर आध्यात्मिक साधक हैं। वह कहते हैं, “मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। शरीर को क्या खिलाना, कब सोना – इन बातों का क्या महत्व?” वह अनियमित खाते हैं, कम सोते हैं, और अपनी बीमारियों का इलाज नहीं कराते। एक दिन वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उनके गुरु आए और कहा, “शरीर भगवान का दिया हुआ मंदिर है। इसकी देखभाल न करना भी एक प्रकार का अहंकार है – ‘मैं शरीर से परे हूँ’। जब तक तुम शरीर में हो, इसका सम्मान करो।”
निष्कर्ष: अनुभवकर्ता की दृष्टि – साक्षी भाव
ये सभी उदाहरण हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाते हैं – हमारे व्यवहार, वाणी, विचार, संबंध, मनोरंजन और स्वास्थ्य के प्रति हमारा दृष्टिकोण ही हमारी आध्यात्मिक यात्रा का निर्धारण करता है।
सोचिए, जब आप सिनेमा हॉल में फिल्म देखते हैं, तो आप पर्दे पर होने वाली घटनाओं के साक्षी होते हैं। आप हँसते हैं, रोते हैं, डरते हैं – लेकिन अंत में आप जानते हैं कि यह सब एक फिल्म है, आप इससे अलग हैं। ठीक इसी तरह, हमारे जीवन में भी, हम अपने व्यवहार, विचार, और भावनाओं के साक्षी हैं।
रामू चाय वाले की कहानी शहर के एक छोटे से चौराहे पर रामू चाय बेचता था। वह हमेशा मुस्कुराता रहता था, चाहे ग्राहक कितने भी अभद्र व्यवहार करें। एक दिन एक प्रोफेसर ने उससे पूछा, “रामू, तुम हमेशा इतने शांत कैसे रहते हो?” रामू ने अपना जवाब देते हुए चाय बनाना जारी रखा और कहा:
“साहब, मैं अपने आप को एक सिनेमा हॉल में बैठा हुआ देखता हूँ। मेरे सामने जीवन का फिल्म चल रहा है – कोई आता है, कोई जाता है, कोई मुझे गाली देता है, कोई तारीफ करता है। मैं सब देखता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं यह सब नहीं हूँ। मैं सिर्फ देखने वाला हूँ।”
प्रोफेसर चौंक गए। उन्होंने पूछा, “तुमने यह कहाँ से सीखा?” रामू ने कहा, “मेरे गुरुजी ने सिखाया। वे कहते हैं, ‘तुम दृष्टा हो, दृश्य नहीं। साक्षी हो, विचार नहीं। अनुभवकर्ता हो, अनुभव नहीं।'”
प्रोफेसर को उस दिन अपने जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान एक साधारण चाय वाले से मिला।
साक्षी भाव से जीवन जीने के कुछ सरल तरीके:
- आज ही से शुरू करें: सुबह उठते ही 5 मिनट शांति से बैठें और महसूस करें कि आप अपने शरीर, मन और भावनाओं के साक्षी हैं।
- दैनिक कार्यों में जागरूकता लाएं: चाहे आप नहा रहे हों, खाना बना रहे हों, या ऑफिस में काम कर रहे हों – महसूस करें कि आप इन सभी क्रियाओं के साक्षी हैं।
- विचारों को देखें, उनसे जुड़ें नहीं: जब भी विचार आएँ, उन्हें बादलों की तरह देखें जो आकाश (आप) में आते-जाते हैं। न उन्हें पकड़ें, न उनसे लड़ें।
- हर शाम समीक्षा करें: दिन भर क्या हुआ, उसे साक्षी भाव से देखें। न खुद की आलोचना करें, न प्रशंसा – सिर्फ देखें।
- प्रकृति का अवलोकन करें: समय-समय पर पेड़, आकाश, नदी या पहाड़ों को देखें। इनकी शांति आपको अपने भीतर के साक्षी से जोड़ेगी।
याद रखें, धार्मिक वृत्तियों को अपनाने और अधार्मिक वृत्तियों से दूर रहने का मतलब यह नहीं है कि आप उन्हें नियंत्रित करें। सच्ची आध्यात्मिकता का अर्थ है – सब कुछ देखना, समझना और फिर भी अपने मूल स्वरूप में स्थित रहना।
अंततः, जैसे-जैसे हम इस साक्षित्व भाव में रहना सीखते हैं, हमारी धार्मिक वृत्तियाँ स्वाभाविक रूप से बढ़ती जाती हैं और अधार्मिक वृत्तियाँ स्वतः ही कम होती जाती हैं। यही सच्ची आध्यात्मिक उन्नति है।




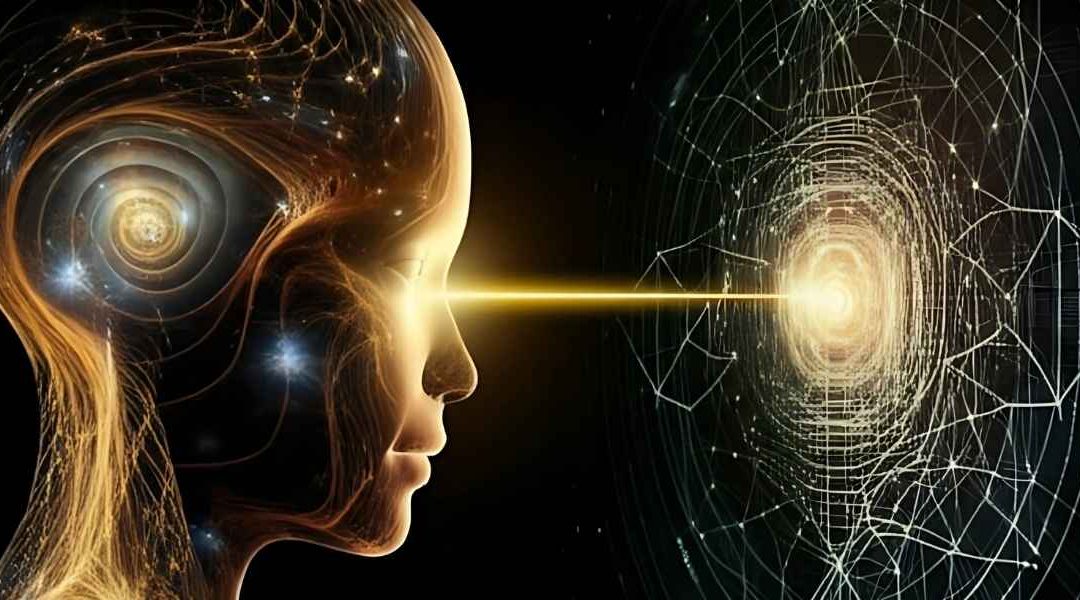

Bahut bahut shukriya
🙏