ॐ असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय॥ (हे प्रभु! मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो॥)
अपरोक्ष अनुभव और तर्क से पहचानें अपना असली स्वरूप
नमस्कार मित्रों! आज हम बात करेंगे आत्मज्ञान की – उस ज्ञान की, जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। यह ज्ञान मार्ग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि जब हम स्वयं को ही नहीं जानते, तो बाकी सब ज्ञान कैसे सार्थक हो सकता है?
आपने कभी सोचा है कि आप वास्तव में हैं क्या? अधिकतर लोग कहेंगे, “मुझे पता है मैं क्या हूं, इसमें बताने की क्या जरूरत है?” लेकिन क्या वाकई हमें पता है? आइए, इस यात्रा पर निकलते हैं, जहां हम अपरोक्ष अनुभव और तर्क के माध्यम से अपने सच्चे स्वरूप को जानेंगे।
ज्ञान मार्ग क्या है?
शुरुआत करते हैं ज्ञान मार्ग को समझने से। ज्ञान मार्ग एक ऐसा आध्यात्मिक रास्ता है, जिसका मुख्य उद्देश्य अज्ञान का नाश करना है। अज्ञान क्या है? वो सभी मान्यताएं, अंधविश्वास, और धारणाएं जिन्हें हमने बिना सोचे-समझे, बिना प्रमाण के मान लिया है। जो दूसरों ने बताया और हमने सच मान लिया।
इस अज्ञान का नाश कैसे होगा? दो साधनों से:
- आपका अपना अनुभव (अपरोक्ष अनुभव)
- आपकी अपनी बुद्धि (तर्क)
ज्ञान मार्ग की खूबी यह है कि यहां किसी किताब या गुरु के वचनों को अंधे होकर नहीं माना जाता, बल्कि स्वयं के अनुभव से सत्य को जाना जाता है। आप जो देखते हैं, अनुभव करते हैं, और तर्क से समझते हैं – वही आपका ज्ञान बनता है।
ज्ञान मार्ग पर चलने से क्या लाभ होते हैं? शांति, सुख, आनंद, बुद्धि का विकास, मुक्ति, स्वतंत्रता – ये सभी फल मिलते हैं। क्योंकि अधिकतर लोग अज्ञान के कारण ही विभिन्न प्रकार के दुखों में फंसे रहते हैं।
ज्ञान मार्ग में तीन प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया जाता है:
- आत्म ज्ञान – मैं क्या हूँ?
- माया का ज्ञान – जगत क्या है?
- ब्रह्म ज्ञान – परम सत्य क्या है?
आज हम आत्मज्ञान पर ध्यान केंद्रित करेंगे, क्योंकि यही तीनों में सबसे मूलभूत और महत्वपूर्ण है।
आत्मज्ञान: मैं क्या हूँ? तत्व क्या है? मैं कौन हूँ?
आत्मज्ञान का अर्थ है अपना तत्व जानना। तत्व क्या होता है? तत्व वह है जो सबसे आवश्यक है, जिसे हटाया नहीं जा सकता। आप में जो चीजें हैं, उनमें से सबसे आवश्यक, सबसे जरूरी क्या है – वही आपका तत्व है। अंग्रेजी में इसे essence कहते हैं।
इसे समझने के लिए एक सरल उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके घर में लकड़ी से बना हुआ टेबल है। इस टेबल का आकार बदला जा सकता है, ऊंचाई बदली जा सकती है, रंग बदला जा सकता है, पॉलिश बदली जा सकती है। आप ड्रावर जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं, पहिए लगा सकते हैं या हटा सकते हैं – ये सब परिवर्तन हो सकते हैं।
लेकिन, अगर टेबल की लकड़ी ही निकाल दी जाए, तो क्या रहेगा? कुछ भी नहीं! इसका अर्थ है कि लकड़ी ही उस टेबल का तत्व है – वह अनिवार्य तत्व जिसके बिना टेबल का अस्तित्व ही नहीं है।
ठीक इसी तरह, हमें यह पता लगाना है कि हमारा तत्व क्या है – वह कौन सा अनिवार्य तत्व है, जिसके बिना हम नहीं रह सकते? और इसे जानने का सबसे अच्छा तरीका है, एक-एक करके उन सभी चीजों को हटाना जो हम नहीं हैं। जो अंत में बचेगा, वही हमारा तत्व है।
मैं क्या नहीं हूँ?
1. वस्तुएं
सबसे पहले, आपके आसपास की वस्तुएँ – फोन, कुर्सी, मेज, किताबें – आप इनमें से कोई नहीं हैं। क्यों? क्योंकि:
- ये आपसे अलग दिखाई देती हैं
- अगर ये बदलें या नष्ट हो जाएँ, तो आप नहीं बदलते या नष्ट नहीं होते
यहाँ हम दो महत्वपूर्ण नियम बना सकते हैं:
- जिसका अनुभव मुझे होता है, वो मैं नहीं हूँ
- जो बदलता है, वो मैं नहीं हूँ
इन दो नियमों का उपयोग करके, हम आगे बढ़ते हैं।
2. शरीर
क्या आप अपना शरीर हैं? शरीर का अनुभव होता है? हाँ। शरीर दिखाई देता है? हाँ। शरीर बदलता है? निश्चित रूप से!
जब आप पैदा हुए थे, तब का शरीर और अब का शरीर एक समान है क्या? बिल्कुल नहीं। शरीर हर पल बदल रहा है – 5 साल की उम्र में था, 10 साल में, 20 साल में, और अब भी – लगातार परिवर्तन। तो हमारे नियम कहते हैं, शरीर मैं नहीं हूँ।
और गहराई से सोचें – क्या आप अपने हाथ हैं? या पैर? या आँखें? या कोई अन्य अंग? अगर किसी का हाथ या पैर न हो, क्या वह अपूर्ण है? कभी नहीं! वह व्यक्ति पूर्ण है, क्योंकि उसका सच्चा स्वरूप इन अंगों से परे है।
हम कहते हैं, “हाथ मेरा है,” “पैर मेरा है,” न कि “मैं हाथ हूँ” या “मैं पैर हूँ”। यह दर्शाता है कि शरीर मेरा है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ।
3. शारीरिक अनुभूतियाँ
शरीर में होने वाली अनुभूतियाँ – जैसे दर्द, भूख, प्यास, नींद, थकान – क्या ये मैं हूँ?
दर्द का उदाहरण लें। जब दर्द नहीं था, तब भी आप थे। जब दर्द हो रहा है, तब भी आप हैं। जब दर्द चला जाएगा, तब भी आप रहेंगे। आप कभी नहीं कहेंगे, “मैं वह दर्द हूँ, और दर्द चला गया तो मैं भी चला गया।”
इसलिए, कोई भी शारीरिक अनुभव आपका तत्व नहीं है। ये आपके अनुभव हैं, आप नहीं।
4. भावनाएँ
भावनाएँ – जैसे डर, गुस्सा, खुशी, दुख, प्रेम, घृणा – ये आती-जाती रहती हैं। कुछ पल पहले आप खुश थे, अब शायद चिंतित हैं, कुछ देर बाद शायद शांत हो जाएँगे।
प्रेम की भावना लें। जब आप किसी प्रियजन से मिलते हैं, तीव्र प्रेम महसूस होता है। कुछ समय बाद, काम में व्यस्त होने पर वह तीव्रता कम हो जाती है। लेकिन आप, जिन्हें यह अनुभव हो रहा है, वही रहते हैं।
तो भावनाएँ भी आपका तत्व नहीं हैं। वे आती-जाती हैं, बदलती हैं, और आप उनके अनुभवकर्ता हैं।
5. विचार
विचारों का क्या? हर सेकंड कई विचार आते और जाते हैं। एक क्षण में आप सोचते हैं कि क्या खाना बनाएँ, अगले क्षण में कार्यालय के काम के बारे में, फिर अपने परिवार के बारे में।
कोई भी विचार स्थायी नहीं है। वे सभी बदलते हैं। इसलिए, विचार भी आपका तत्व नहीं हो सकते।
6. इच्छाएँ
इच्छाएँ भी निरंतर बदलती रहती हैं। एक नया फोन चाहिए, फिर वह मिल गया, तो अब नई कार चाहिए, फिर बड़ा घर, फिर अच्छा स्वास्थ्य… यह क्रम कभी खत्म नहीं होता।
इच्छाएँ परिवर्तनशील हैं, जबकि आप, जिन्हें इन इच्छाओं का अनुभव हो रहा है, वही रहते हैं। तो इच्छाएँ भी आपका तत्व नहीं हैं।
7. स्मृति (मेमोरी)
स्मृति भी बदलती रहती है। कुछ याद रहता है, कुछ भूल जाते हैं। आपको याद है कि आपने कल क्या खाया था? शायद हाँ। और एक महीने पहले? शायद नहीं।
स्मृति चली गई, लेकिन आप वही हैं। इसलिए, स्मृति भी आपका तत्व नहीं है।
आपका नाम, आपकी पढ़ाई-लिखाई, आपका पेशा, आपके रिश्ते – ये सब स्मृति में हैं। अगर इन स्मृतियों को हटा दिया जाए, तो आप कहेंगे “मुझे याद नहीं,” लेकिन आप फिर भी वही रहेंगे।
8. स्त्री, पुरुष या किन्नर होना
स्त्री, पुरुष या किन्नर होना – ये शरीर के प्रकार हैं। और हम देख चुके हैं कि शरीर हमारा तत्व नहीं है। साथ ही, इनसे जुड़े संस्कार और भूमिकाएँ स्मृति और संस्कृति में हैं, जो भी हमारा तत्व नहीं हैं।
इसलिए, आपका तत्व न स्त्री है, न पुरुष, न किन्नर – यह इन सबसे परे है।
9. सपने
रात में सपने में, आपको अपनी एक छवि दिखाई देती है। वहां भी शरीर होता है, भावनाएँ होती हैं, विचार होते हैं। लेकिन जागने पर आप जानते हैं कि वह सब आप नहीं थे। वे केवल मानसिक अनुभव थे।
इसलिए, न तो जागृत अवस्था, न स्वप्न अवस्था, न सुषुप्ति (गहरी नींद) की अवस्था – इनमें से कोई भी आपका तत्व नहीं है। आप इन सभी अवस्थाओं के अनुभवकर्ता हैं।
तो मैं क्या हूँ?
हमने जगत के, शरीर के और मन के सभी अनुभवों को देख लिया। इनमें से कोई भी हम नहीं हैं। लेकिन फिर भी हम हैं, अस्तित्व में हैं। तो हम क्या हैं?
हम वह हैं जो इन सभी अनुभवों का अनुभव करता है – साक्षी, द्रष्टा, अनुभवकर्ता।
सभी बदलते हुए अनुभवों के बीच एक स्थिर तत्व है – जो देखता है, जानता है, अनुभव करता है, लेकिन स्वयं नहीं बदलता। वही हमारा तत्व है, वही हम हैं। इसे ही “साक्षी” कहते हैं।
साक्षी का अर्थ है – सभी अनुभवों का साक्षी, द्रष्टा। मैं जगत, शरीर और मन के सभी अनुभवों का साक्षी हूँ। यह साक्षी मेरा तत्व है, यही सबसे आवश्यक है। इसे हटा दें तो कुछ नहीं बचता।
साक्षी के गुण
1. निराकार और अपरिवर्तनशील
साक्षी का कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है। अगर इसका कोई रूप होता, तो यह दिख जाता और फिर अनुभव बन जाता। यह न भौतिक है, न मानसिक – यह परा-भौतिक और परा-मानसिक है।
साक्षी अपरिवर्तनशील है – यह कभी नहीं बदलता। यदि यह बदलता, तो यह आता-जाता अनुभव हो जाता, और हम नहीं होता।
2. अजन्मा, अजर, अमर
जन्म कैसे होता है? जब मिट्टी से घड़ा बनता है, तो घड़े का जन्म होता है – एक पदार्थ (मिट्टी) बदलकर एक नया रूप (घड़ा) लेता है। जन्म के लिए तीन चीजें जरूरी हैं: पदार्थ होना, बदलाव होना, और आकार लेना।
साक्षी में इनमें से कोई भी नहीं है – न पदार्थ है, न बदलाव है, न आकार है। इसलिए, साक्षी का जन्म नहीं होता – यह अजन्मा है।
ठीक इसी तरह, साक्षी बूढ़ा नहीं होता, इसे रोग नहीं होता – यह अजर है, अक्षय है। और क्योंकि इसका जन्म नहीं होता, इसलिए इसकी मृत्यु भी नहीं होती – यह अमर है।
हम शरीर की उम्र बढ़ने के साथ बदलते महसूस करते हैं, लेकिन अगर गहराई से देखें, तो वह अनुभवकर्ता जो 5 साल की उम्र में था, वही 50 साल की उम्र में भी है। साक्षी भाव कभी नहीं बदलता।
3. मुक्त और स्वतंत्र
जिसका जन्म नहीं होता, उसका पुनर्जन्म भी नहीं हो सकता। साक्षी जन्म-मृत्यु के चक्र से परे है – यह पहले से ही मुक्त है।
साक्षी को किसी जेल में बंद नहीं किया जा सकता, किसी पिंजरे में नहीं रखा जा सकता, किसी रस्सी से नहीं बांधा जा सकता। इसे मारा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता। यह बंधन-मुक्त है, स्वतंत्र है।
शरीर बंधन में हो सकता है, लेकिन साक्षी भाव सदा मुक्त है।
4. शांत और आनंदमय
साक्षी में कोई दर्द नहीं है, कोई सुख-दुख नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई चिंता नहीं है। यह शांत है।
साक्षी को कोई शिकायत भी नहीं है – यह केवल देखता है। इसीलिए यह आनंदमय है। आनंद का अर्थ यहाँ खुशी या हंसी नहीं, बल्कि पूर्ण शांति और संतुष्टि है।
गहरी नींद में जब कोई विचार या चिंता नहीं होती, वह शांति का अनुभव साक्षी का स्वभाव है – हमेशा शांत, हमेशा आनंदमय।
5. सर्वव्यापी और एक
क्या हर व्यक्ति में अलग-अलग साक्षी है? नहीं! यदि दो वस्तुओं के गुण मिलते हैं और दोनों के बीच में कोई सीमा नहीं है, तो वे एक ही होती हैं।
जैसे तालाब के दाएँ और बाएँ हिस्से में पानी एक ही है, वैसे ही सभी में साक्षी एक ही है। सभी साक्षियों के गुण समान हैं और उनके बीच कोई सीमा नहीं है। इसलिए, एक ही साक्षी है जो सभी में व्याप्त है।
यही अध्यात्मिक प्रेम है – एक होने का अनुभव। सभी का तत्व एक ही है, मैं ही सभी में हूँ।
आत्मज्ञान का सारांश
तो आत्मज्ञान क्या है? यह जानना कि:
- मैं जगत, शरीर, वस्तु, मन – इनमें से कोई भी नहीं हूँ
- मैं कोई अनुभव नहीं हूँ
- मुझमें परिवर्तन नहीं है – मैं नित्य हूँ
- मैं निराकार हूँ, अरूप हूँ
- मैं परा-भौतिक, परा-मानसिक हूँ
- मैं अजन्मा, अजर, अमर हूँ
- मैं बंधन-मुक्त, जन्म-मृत्यु के चक्र से मुक्त हूँ
- मैं शांत, आनंदमय हूँ
- मैं प्रेम हूँ – सभी में मैं ही व्याप्त हूँ
इस ज्ञान को केवल पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है। इसे अपने अनुभव से जांचना होगा। घर में बैठकर इस पर मनन कीजिए, विचार कीजिए, और देखिए कि क्या यह सत्य है।
जब आप जान लेते हैं कि आप साक्षी हैं, सभी अनुभवों के द्रष्टा हैं, तब आपको मुक्ति, शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। यही सच्चा आत्मज्ञान है।
आशा है, यह लेख आपके आत्मज्ञान की यात्रा में सहायक सिद्ध होगा। याद रखिए, यह ज्ञान केवल बौद्धिक नहीं, बल्कि अनुभवजन्य है। इसे स्वयं अनुभव करें, तर्क से जांचें, और अपने जीवन में उतारें।
क्या आपके मन में कोई प्रश्न है? क्या आपने कभी आत्मज्ञान का अनुभव किया है? अपने विचार और अनुभव हमारे साथ टिप्पणी में साझा करें।




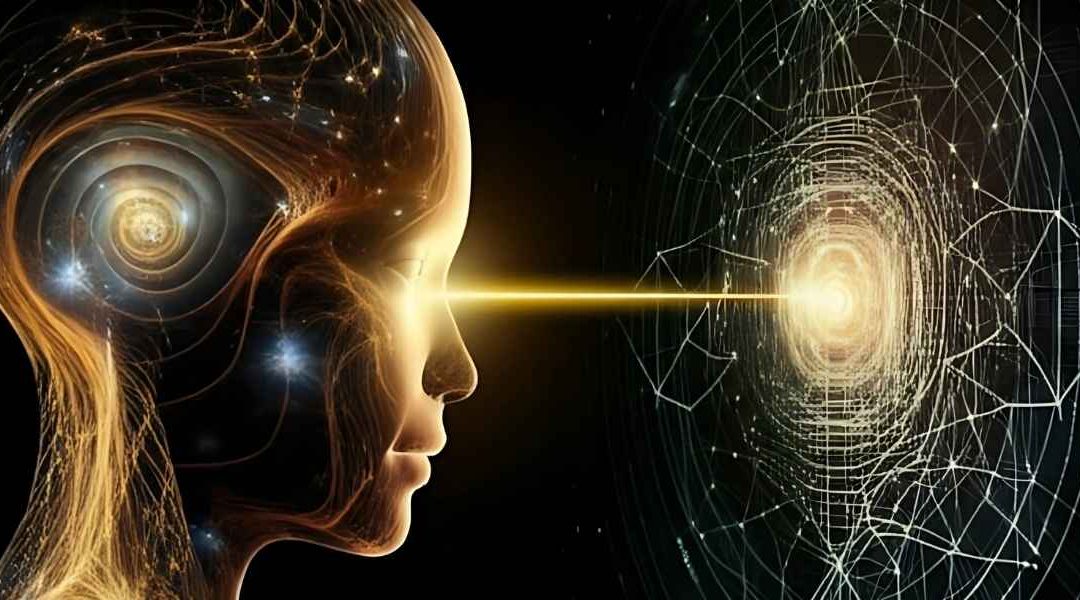

0 Comments